गोवर्धन यादव
ईश्वर की सबसे सुन्दर कृति यदि कोई है, तो वह प्रकृति है. इसका सांगोपान वर्णन करना इतना आसान नहीं हैं, जितना की हम समझते हैं. इसकी सुन्दरता में चार चांद लगाते हैं रंग। सूर्य की लालिमा हो या खेतों की हरियाली, आसमान की लालिमा हो या मेघों की कालिमा, बारिश के बाद बिखरती इन्द्रधनुष की अनोखी छटा और ऐसे ही अनगिनत खूबसूरत नजारें, जो हमारे अंतर्मन, आत्मा, और इन्द्रियों को खुशी प्रदान करते है, इस आनंद का राज है, रंगो की अनुभूति रंग हमारे परिवेश में इस तरह घुले-मिले हैं कि हम उन्हें अलग से देखने का प्रयास ही नहीं करते. रंगों का हमारे जीवन में दृश्य-अदृश्य रूप से हमारे भावों और विचारों पर प्रभाव पड़ता है,क्योंकि रंगों में आत्मिक भावना को संप्रेषित करने का सामर्थ्य है. मानव जीवन रंगो के बिना उदास और सूना है.
प्रकृति के साथ मेल
रंगों से हमारा रिश्ता अनायास ही नहीं है, धार्मिक आस्थाओं से लेकर वैज्ञानिक आधारों तक यही कहते हैं कि रंगों को धारण कर हम ईश्वर की कृति प्रकृति से करते हैं. वासंती रंग हमें वसंत के फूलों से तारतम्य बनाने में सहायक होते हैं. और हरा रंग हरी-हरी पत्तियो से. नीला रंग तो आसमान का आईना है, तो लाल रंग सुबह-शाम की लालिमा से हमारा रिश्ता जोड़ता है. रंगों से हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं. और हम फिर से प्रकृति के फूल-पत्ते, पेड़ों,जंतुओं से अपना प्रगाढ़ रिश्ता बनाना चाहते हैं. इसलिए रंग हमारी संस्कृति को प्रकृति से जोड़ते हैं. जहाँ प्रकृति में रंग कम होते हैं, वहाँ रंगों से उस रंग की पूर्ति हो जाती है. उदाहरण के तौर पर राजस्थान पूरी दुनिया में रंगीलो राजस्थान के नाम से विख्यात है, जबकि सच्चाई है कि वहाँ पानी की बेहद कमी है और कभी धूसर और मटमैले रेत के टीलों की जननी है, जिसकी वजह से चार और रंगों का खासा अभाव महसूस किया जाता है. ऐसे में रंगों की कमी की पूर्ति के लिए लोगों के द्वारा पहनी जाने वाली रंग-बिरंगी वेश-भूषा से की जाती है.
रंगो की गाथा
ईश्वर ने मनुष्य को ज्यादा रंगीन नहीं बनाया. लेकिन आदिमकाल से मनुष्य अपने को रंगने के लिए कोई न कोई कारण ढूंढता आया है. आदिम समाजों में धार्मिक अनुष्ठान हों या सामुहिक नृत्य या युद्ध का मौका लोग अपने चेहरे और शरीर पर कई तरह के रंग लगाकर, सिर पर रंग-बिरंगे पंखों को धारण करके, मुखौटे लगाकर अपनी खुशी का इजहार करते थे,. रंगों को प्राचीनकाल से अब तक अनेक प्रतीकात्मक रूप में लिया जा रहा है. जिसका दार्शनिक, सामाजिक और धार्मिक उद्देश्य रहा है. विभिन्न वेदों, पुराणों, ग्रंथों यहां तक कामसूत्र में भी रंगों, उसमें मिलने वाले महत्व का उल्लेख मिलता है. साथ ही कवियों के अनेक काव्य साहित्यों मे भी रंगों का गुणगान किया गया है.तंत्र सिद्धांत और साधना के अंतर्गत समस्त भौतिक जगत का निर्माण जिन पांच तत्वों से मिलकर हुआ है वह है-पृथ्वी तत्व-पीग, जल तत्व-श्वेत,अग्नि तत्व-रक्त, वायु तत्व-श्याम, और आकाश तत्व. रामायण, महाभारत, देवताओं, राजा-रानियों, राजकुमारों आदि के पहनावे में भी रंगों का चयन का महत्व माना गया है. पौराणिक काल से ही हमारे देवी-देवताओं को भी कुछ खास रंग विशेष प्रिय है. यहां तक कि ये विशेष रंगों से पहचाने भी जाते हैं. मां लक्ष्मी को लाल रंग प्रिय है. भगवान श्री कृष्ण को पीतांबरधारी कहते हैं, क्योंकि ये पीले रंग के वस्त्रों से सुशोभित रहते हैं. शनिदेव को काला रंग प्रिय है.
टेसू के फूलों के रंग
प्रारंभ में लोग प्राकृतिक रंगों को ही उपयोग में लाते थे. उल्लेखनीय है कि मोहन जोदड़ों और हड़प्पा की खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता की जो चीजें मिलीं उनमें ऐसे बर्तन और मूर्तियाँ भी थीं, जिन पर रंगाई की गई थी. उसमें एक लाल अरंग का टुकड़ा भी पाया गया. विशेषज्ञों के अनुसार, इस पर मजिठ या मजिष्ठा की जड़ से तैयार किया गया रंग चढ़ाया गया था. हजारों वर्षों तक मजीठ की जड़ और बक्कम वृक्ष की छाल लाल रंग का मुख्य स्त्रोत रही. पीपल,गूलर, और पाकड जैसे वृक्षों की छाल से लाल रंग का मुख्य स्त्रोत रही.पीपल, गूलर,और पाकड़ जैसे वृक्षों पर लगने वाली लाख की कृमियों की लाह से महावर रंग तैयार किया गया जाता था.पीला रंग और सिंदूरी हल्दी से प्राप्त होता था. धीरे-धीरे प्राकृतिक रंगो को तैयार करने के लिए दूसरे साधनों का सहारा लिया जाने लगा.टेसू के फूलों की मदद से पीला और नारंगी रंग बनाया जाता था. लाल रंग के लिए लाल अनार के छिलकों या सूक्शे सूर्ख लाला गुलाब की पंखड़ियों को पानी में उबालकर रंग तैयार किया जाता था. नीले रंग के लिए नील के पेड़ के फल या जकांड़ा के सूखे फूलों को पीसकर पानी में घोला जाता था. हरा रंग बनाने के लिए पुदिना, धनिया, पिपरमिंट, पालक या सोसोखी मेहंदी के पाऊडर को पानी में घोला जाता था. पीले रंग के लिए सूखे गेंदे के फूलों की पंखड़ियों, हल्दी या बेसन के पाउडर का प्रयोग किया जाता था.बैंगनी रंग के लिए शलजम को कद्दुकस करके पानी में भिंगोया जाता था या प्याज के सूखे पत्तों को निकालकर पानी में भिंगोकर रंग बनाया जाता था. भूरे रंग के लिए कत्थे को काम में लाया जाता था
रंगो का विस्तार
पस्चिम में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपड़ा उद्योग का तेजी से विकास हुआ. रंगो की खपत बढ़ी. प्राकृतिक रंग सीमित मात्रा में उपलब्ध थे. इसलिए बढ़ी हुई मांग की पूर्ती प्राकृतिक रंगों से संभव नहीं थी. ऐसी स्थिति में कृत्रिम रंगो की तलाश शुरू हुई. तमाम प्रयोगों के बाद 1856 में तैयार हुए कृत्रिम रंग को मोच कहा गया. आगे चलकर 1860 में रानी रंग, 1862 में अनलोन नीला और अनलोन काला रंग,1865 में बिस्माई भूरा,1880 में सूती काला जैसे रासायनिक रंग, 1882 में नीला रंग अस्तित्व में आ चुके थे. 1867 में रानी रंग (मर्जेंटा) का आयात किया था. 1872 में जर्मन रंग विकेताओं के लिए आया.
रंगो में छुपे अर्थ
हर रंग में कुछ न कुछ अर्थ छुपा होता है. किसी को उपहार देना हो तो इसके चुनाव का महत्वपूर्ण भूमिका रंगों की ही होती है. रंगो की अपनी गुप्त ऊर्जा होती है, जो गतिशीलता प्रदान करने के साथ ही हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में सहयोग करती है. यही वजह है कि विज्ञापनों में रंगों के द्वारा कई बार कठिन संदेशोंको भी कुछ ही क्षणों में सहज ही समझा जा सकता है.व्यक्तियों, घटनाओं, अवस्थाओं, यहांम्तक कि दुगंध और दुर्गंध को भी चित्रों और चित्रों में भरे अलग-अलग रंगों के माध्यम से दूबसूरती के साथ अभिव्यक्त किया जा सकता है. रंग अलग-अलग वर्गों को अपनी तरह से आकर्षित करते हैं. छोटे बच्चों को रंग-बिरंगे खिलौने अपनी ओर खींचते हैं. खुशी और दुःख को फूलों के रंगों के द्वारा व्यक्त किया जाता है. मकानों, दुकानोंम माल्स, कपड़ों आदि की सुंदरता भी रंगों पर निर्भर करती है. हमारे संसार का शायद ही कोई ऐसा पहलू है जो रंगो में जादू से मुक्त हो.













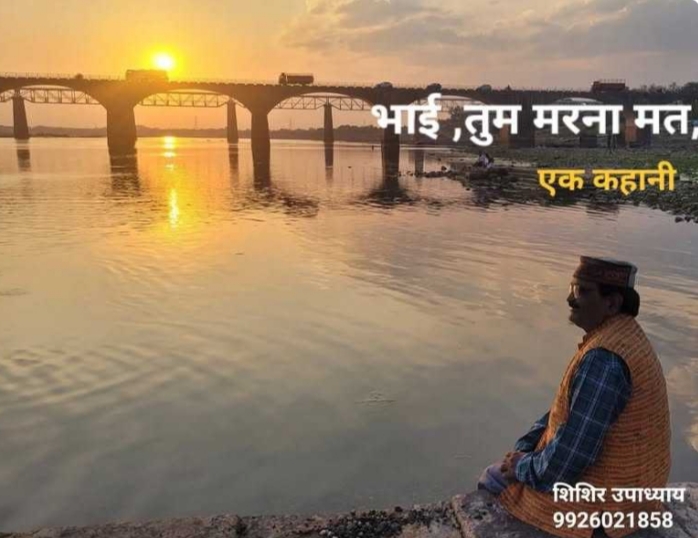


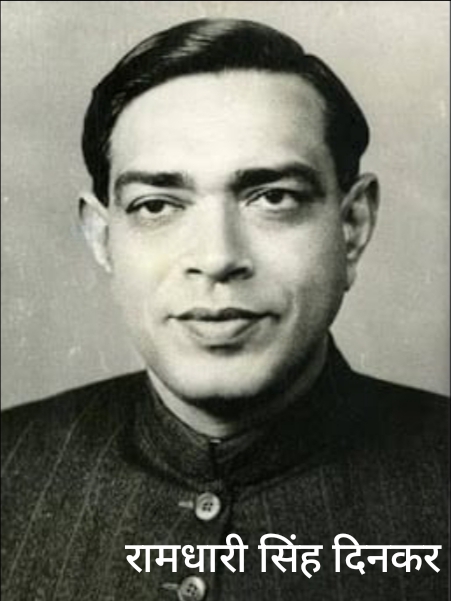
Leave a Reply