महेश अग्रवाल
योग गुरु महेश अग्रवाल नें बताया कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है — वह एक चलता-फिरता ब्रह्माण्ड है। उसमें वह सब विद्यमान है जो इस विराट विश्व में है। किंतु इस सत्य को जानने के लिए उसे भीतर उतरना पड़ता है, आत्मानुभूति के उस गहरे स्रोत में जहाँ कुण्डलिनी शक्ति सुषुप्त पड़ी है। यही वह रहस्यमयी शक्ति है, जो जागने पर मनुष्य को सामान्य से असामान्य, सीमित से असीम, भौतिक से दिव्य बना देती है। कुण्डलिनी योग का अर्थ केवल योगिक आसनों का अभ्यास नहीं है, यह मनुष्य की चेतना को मूल से सहस्रार तक आरोहण कराने की एक दिव्य प्रक्रिया है — जो अज्ञान से ज्ञान, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाती है।
कुण्डलिनी शब्द का अर्थ : “कुण्ड” से “कुण्डलिनी” तक
बहुत लोग मानते हैं कि “कुण्डलिनी” का अर्थ “कुण्डल” अर्थात लपेटा या फेरा होता है, परंतु शास्त्रीय दृष्टि से इसका अर्थ इससे कहीं गहरा है। संस्कृत में “कुण्ड” का अर्थ है – गहरा स्थान, गढ्ढा या एक केंद्र। और जो शक्ति उस कुण्ड में स्थित है, वही कहलाती है कुण्डलिनी। ऋषियों के अनुसार मानव मस्तिष्क और मेरुदण्ड के संयोग क्षेत्र में एक सूक्ष्म केन्द्र है जहाँ यह प्रमुख केंद्रीय शक्ति सुषुप्त पड़ी है। यह शक्ति ही हमारे समस्त मानसिक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक विकास का स्रोत है।जब साधना के माध्यम से यह शक्ति जागृत होती है, तब मस्तिष्क के वे केन्द्र जो अब तक निष्क्रिय पड़े हैं, सक्रिय हो उठते हैं। यही अवस्था “चेतना का जागरण” या “कुण्डलिनी आरोहण” कहलाती है।
कुण्डलिनी जागरण का प्रभाव : आंतरिक रूपान्तरण का विस्फोट
जब कुण्डलिनी जागृत होती है, तो साधक के भीतर केवल अनुभव नहीं, एक अस्तित्व-परिवर्तन घटित होता है। जीवन में एक अद्भुत आनन्द, एक स्थायी शांति और दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगता है। नैतिकता, धर्म, संयम और चारित्रिक जीवन में परिवर्तन आता है, किंतु इससे भी बड़ा परिवर्तन साधक की अनुभूति के स्तर पर होता है। साधक की सीमित सामाजिक चेतना अब सार्वभौमिक चेतना में परिवर्तित हो जाती है। वह अब केवल व्यक्ति नहीं रह जाता, वह “विराट का अंश” बन जाता है। इस अवस्था में मन के अनुशासन और समाज के भय का स्थान आत्म- नियंत्रण और दिव्य प्रेरणा ले लेती है।
आध्यात्मिक जागृति और समाज की दृष्टि
इतिहास साक्षी है कि जब किसी महापुरुष की कुण्डलिनी शक्ति जागृत होती है, तो उसके विचार समाज के सामान्य सोच से परे हो जाते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध , मीरा, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद — सभी की बातें कभी समाज को असंगत लगीं, क्योंकि वे सामान्य नहीं, चेतना की उच्च अवस्था से बोलते थे। कुण्डलिनी-जागृत व्यक्ति जब बोलता है, तो उसके शब्द आत्मा की गहराइयों से निकलते हैं। साधारण व्यक्ति उसे ‘पागलपन’ समझ लेता है, परन्तु वास्तव में वह ‘आध्यात्मिक उन्माद’ होता है, जिसमें आत्म-नियंत्रण का अभाव नहीं, बल्कि परम आत्म-प्रेरणा का प्रवाह होता है।
क्या कुण्डलिनी जागरण खतरनाक है?
बहुत लोग कहते हैं कि “कुण्डलिनी जागरण खतरनाक होता है।” परंतु यह केवल भय का भ्रम है। वास्तव में कुण्डलिनी जागरण में कोई वास्तविक खतरा नहीं है। हाँ, जब चेतना ऊर्ध्वगामी होती है, तब कुछ शारीरिक या मानसिक परिवर्तन अवश्य होते हैं — जैसे कभी मन अशांत होना, प्यास लगना, नींद का कम होना, भावनात्मक उतार-चढ़ाव आदि। पर ये सब अस्थायी हैं और स्थिर होने पर साधक पहले से अधिक शांत, संतुलित और जागरूक हो जाता है। वास्तव में रोजमर्रा के जीवन में हम कुण्डलिनी मार्ग की अपेक्षा अधिक खतरनाक स्थितियों से गुजरते हैं — सड़क पार करते हुए, हवाई यात्रा में, या वाहन चलाते समय। इनकी तुलना में कुण्डलिनी साधना का मार्ग अधिक सुरक्षित और लाभदायक है — यदि उसे सही विधि से और योग्य गुरु के निर्देशन में किया जाए।
कुण्डलिनी योग और क्रियायोग : एक ही धारा के दो नाम
क्रियायोग वह विज्ञान है जो कुण्डलिनी शक्ति को जगाने के लिए विकसित किया गया है। जो भी अभ्यास कुण्डलिनी जागरण में सहायक होता है — प्राणायाम, बंध, मुद्रा, ध्यान या मंत्रजप — सब क्रियायोग के अंतर्गत आते हैं। कुण्डलिनी योग इस ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया है, जबकि क्रियायोग उसका व्यवस्थित वैज्ञानिक रूप। कुण्डलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में रहती है। जब साधक ध्यान, प्राणायाम और क्रियायोग के द्वारा उसे जागृत करता है, तो वह मेरुदण्ड के सूक्ष्म नाड़ियों (इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना) के मार्ग से ऊपर सहस्रार तक पहुँचती है। यही आरोहण आत्म-साक्षात्कार या ईश्वर प्राप्ति की चरम अवस्था है। सभी योगपद्धतियाँ — राजयोग, भक्तियोग, कर्मयोग, ज्ञानयोग — अंततः इसी जागरण की ओर ले जाती हैं।
जागरण का सुगम मार्ग : सेवा, भक्ति और साधना
कुण्डलिनी जागरण का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नशे, भाँग, गाँजा, एल.एस.डी. जैसी औषधियाँ केवल तंत्रिका-तंत्र को उत्तेजित करती हैं, परंतु चेतना को नहीं। वास्तविक जागरण केवल शुद्ध साधना, निष्काम कर्म, और भक्ति से ही संभव है। “कीर्तन, प्राणायाम और निःस्वार्थ सेवा — ये कुण्डलिनी जागरण के सरलतम साधन हैं।” कुण्डलिनी शक्ति किसी यांत्रिक प्रक्रिया से नहीं, बल्कि हृदय की निर्मलता से जागती है। जब मन में सात्त्विकता, दया, संयम, सेवा और सत्य का प्रकाश भर जाता है, तब यह शक्ति स्वयं उठ खड़ी होती है। इसलिए सर्वोत्तम मार्ग है — कर्मयोग + भक्तियोग + राजयोग + ज्ञानयोग का समन्वय।यही चारों मिलकर साधक के भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं।
क्या जागरण मूलाधार से ही आरम्भ होता है?
अधिकांश परंपराओं में कहा गया है कि कुण्डलिनी जागरण मूलाधार चक्र से आरम्भ होता है, लेकिन यह कोई अपरिवर्तनीय नियम नहीं है। हर व्यक्ति की चेतना अलग होती है, और कुछ में जागरण किसी अन्य चक्र — जैसे अनाहत या आज्ञा — से भी प्रारंभ हो सकता है। हर व्यक्ति के कुछ चक्र दूसरे की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं। अनुभव बताते हैं कि साधक को जहाँ सहजता से ध्यान लग जाए, वहीं से अभ्यास आरम्भ करना चाहिए। यदि वहाँ से शक्ति का संचार होता है, तो समझना चाहिए कि वही उसका जागरण-बिंदु है। धीरे-धीरे जब ऊर्जा ऊपर उठती जाती है, तो सभी चक्र क्रमशः प्रकाशित होने लगते हैं।
क्या चक्रों की आंशिक जागृति सम्भव है?
हाँ, बिना पूर्ण कुण्डलिनी जागरण के भी चक्रों की आंशिक जागृति संभव है। अत्यधिक भय, गहन भावनात्मक आघात या गहन ध्यान की स्थिति में भी कुछ चक्र सक्रिय हो जाते हैं।स्वाधिष्ठान चक्र (जो वासनाओं और सृजन से सम्बद्ध है) अक्सर पहले जागृत होता है, जबकि अनाहत और विशुद्धि जैसे उच्च चक्र विरले ही सक्रिय होते हैं। इन आंशिक जागरणों से कुछ विचित्र स्वप्न, अनुभूतियाँ या ऊर्जा का कंपन महसूस हो सकता है, परन्तु यह कोई असामान्य बात नहीं। यदि साधक संयम रखे, तो ये अनुभव उसे उच्च साधना की ओर प्रेरित कर सकते हैं।
जागरण की अनजानी अवस्था : जब साधक को स्वयं पता न चले
कभी-कभी कुण्डलिनी जागृत हो जाती है और साधक स्वयं यह नहीं जान पाता कि उसके भीतर क्या घटित हो रहा है। ऐसी स्थिति में वह अजीब व्यवहार करने लगता है, जिसे लोग “पागलपन” समझ लेते हैं। वास्तव में वह शक्ति-संचार को संभाल नहीं पाता। योग परंपरा कहती है — “कुण्डलिनी जागरण के बाद गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है।” उदाहरणस्वरूप, एक बार एक युवा साधक में चक्रों का स्वतः जागरण हो गया था, और वह नियंत्रण खो बैठा। योगनिद्रा और गुरु-कृपा से जब उसे संतुलन मिला, तब उसकी साधना पुनः स्थिर हो पाई। इसलिए यह मार्ग केवल ज्ञान नहीं, संरक्षण भी चाहता है।
क्या नसबंदी के बाद भी कुण्डलिनी जागरण संभव है?
हाँ, कुण्डलिनी जागरण शारीरिक क्रियाओं पर नहीं, ऊर्जा-संवेदनाओं पर आधारित है। नसबंदी या शारीरिक अवरोध इससे संबंधित नहीं है। हठयोग में सिद्धासन जैसा आसन विशेष रूप से इस क्षेत्र की ऊर्जाओं को नियंत्रित करने हेतु बताया गया है, जिससे निम्न स्तर की संवेदनाएँ उच्च दिशा में प्रवाहित हो सकें।
पशु और कुण्डलिनी
कुण्डलिनी केवल मनुष्य में ही नहीं, प्रत्येक जीव में विद्यमान है।
अंतर केवल स्तर का है। पशुओं में यह शक्ति मूल प्रकृति (निम्न स्तर) पर क्रियाशील रहती है, जबकि मनुष्य में यह मध्य स्तर (बौद्धिक-आध्यात्मिक) पर स्थित है। महान योगी जब अतीन्द्रिय चेतना को प्राप्त करते हैं, तो यह शक्ति उच्चतम स्तर तक पहुँच जाती है। इसीलिए कहा गया — “देवता, मनुष्य और पशु — तीनों में वही शक्ति है, फर्क केवल उसके जागरण-स्तर में है।”
क्या चक्रों के जागरण से मिलने वाली प्रतिभा स्थायी रहती है?
कभी-कभी किसी चक्र का जागरण अस्थायी होता है — जैसे दूरश्रवण (टेलीपैथी), दूरदर्शन या अन्य योगिक शक्तियाँ कुछ समय तक सक्रिय रहती हैं और फिर सुषुप्त हो जाती हैं। परंतु जब साधक साधना में निरंतरता रखता है, तो ये शक्तियाँ स्थायी रूप से उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाती हैं। किन्तु ज्ञानी योगियों ने हमेशा चेताया है – “सिद्धियाँ मार्ग की सीढ़ियाँ हैं, लक्ष्य नहीं।”
सकारात्मक और नकारात्मक अनुभव
कुण्डलिनी के जागरण के समय सकारात्मक (दिव्य) या नकारात्मक (कष्टदायक) अनुभव हो सकते हैं। परंतु ये गुण कुण्डलिनी में नहीं, बल्कि साधक के मनोभावों और कर्म- संस्कारों में निहित होते हैं। यदि साधक का जीवन सात्त्विक, संयमी और मन शांत है, तो जागरण का अनुभव सुखद और प्रकाशमय होगा। यदि मन वासनाओं, भय या कुंठाओं से ग्रस्त है, तो वही ऊर्जा विक्षोभ के रूप में प्रकट होगी। अतः कुण्डलिनी साधना से पहले मन की शुद्धि आवश्यक है – कर्मयोग, भक्ति, ध्यान, प्रार्थना और निःस्वार्थ सेवा के माध्यम से।
कुण्डलिनी पार करते समय भय या पीड़ा क्यों होती है?
स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर उठते समय साधक को दर्द नहीं, बल्कि हल्का भय अनुभव हो सकता है — क्योंकि वह अब ज्ञात जगत से अज्ञात की ओर बढ़ रहा होता है। परंतु यह भय अस्थायी है, और उसके पार होते ही आनंद, प्रसन्नता और स्थिरता की अनुभूति होती है। यह जीवन की सबसे सुखद, सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है।
अचानक जागरण होने पर भ्रम क्यों होता है?
जैसे सौ वर्ष पहले कोई तेज रफ्तार वाहन देखता तो चक्कर खा जाता, वैसे ही अचानक हुई आध्यात्मिक गति भी साधक को भ्रमित कर सकती है। परंतु यदि उसने पूर्व में योगाभ्यास किया है, तो वह इन परिवर्तनों को सहजता से ग्रहण कर लेता है।इसलिए क्रमिक अभ्यास — हठयोग, प्राणायाम, ध्यान, जप, कीर्तन — ये सभी कुण्डलिनी जागरण की तैयारी हैं।
ब्रह्माण्डीय ऊर्जा और कुण्डलिनी
ब्रह्माण्डीय ऊर्जा पृथ्वी पर मनुष्य के माध्यम से प्रकट होती है।जब साधक की कुण्डलिनी शक्ति जागृत होती है, तो उसका मस्तिष्क “सुपर माइंड” बन जाता है। ऐसे ही योगियों और महात्माओं के माध्यम से यह ब्रह्माण्डीय चेतना पृथ्वी पर प्रवाहित होती रहती है। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में सामंजस्य, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है।
नशीले पदार्थ और झूठा जागरण
कुछ लोग भाँग, हशीश या अन्य नशे का सेवन कर “अनुभव” पाने की कोशिश करते हैं। इनसे मन तात्कालिक रूप से सम्मोहन की अवस्था में पहुँच जाता है, किंतु वह चेतना का जागरण नहीं होता। जागरण में चेतना का विकास होता है, जबकि नशे में चेतना का लोप होता है। ऐसे अनुभव केवल भ्रम हैं — न ज्ञान, न शक्ति, न मुक्ति देते हैं। वास्तविक जागरण में शक्ति, संतुलन और दिव्य दृष्टि — तीनों एक साथ विकसित होते हैं।
शरीर और मन की शुद्धि : साधना की पूर्व तैयारी
यदि शरीर शुद्ध नहीं है, तो कुण्डलिनी जागरण से असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। पाचन, रक्त-संचार, श्वसन, और नाड़ी-मण्डल की शुद्धि आवश्यक है। इसके लिए शाकाहारी आहार, प्राणायाम, और हठयोग अनिवार्य हैं। लगभग छह माह तक शुद्ध आहार और नियमित साधना से शरीर जागरण योग्य बन जाता है। मानसिक शुद्धि विचारों से आती है। ईर्ष्या, क्रोध, भय, चिन्ता, आसक्ति जैसे विचार विषाक्त हार्मोन उत्पन्न करते हैं, जो मस्तिष्क को दूषित करते हैं। अतः साधक को मन के इन ‘मलों’ से मुक्त होना आवश्यक है। यही “चित्तशुद्धि” कुण्डलिनी जागरण का वास्तविक आधार है।
कुण्डलिनी जागरण के अनुभव
जब कुण्डलिनी जागृत होती है, तो साधक को ऊर्जा का एक तेज़, विद्युतमय कंपन अनुभव होता है। मेरुदण्ड के नीचे से ऊपर की ओर एक धारा-सी उठती है। कभी यह प्रकाश के रूप में, कभी कंपन के रूप में, तो कभी आंतरिक ध्वनि के रूप में अनुभव होती है। कभी-कभी बाँसुरी, मृदंग, मोरपंख या ओंकार जैसी अनाहत ध्वनि सुनाई देती है। यह अनुभव बिना किसी बाहरी स्रोत के होता है — और यही संकेत है कि जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।
भीतर की यात्रा, बाहर का प्रकाश
कुण्डलिनी का जागरण कोई अलौकिक जादू नहीं — यह आत्मा के भीतर की यात्रा है। यह हमें हमारे भीतर छिपे हुए परमात्मा से मिलाने की प्रक्रिया है। जिस दिन साधक इस ऊर्जा के प्रवाह को सहस्रार तक पहुंचा देता है, उस दिन वह “योगी” नहीं — “योगमय” हो जाता है। उसका जीवन आनंद, ज्ञान और सेवा का संगम बन जाता है।
लेखक के ये अपने विचार हैं।














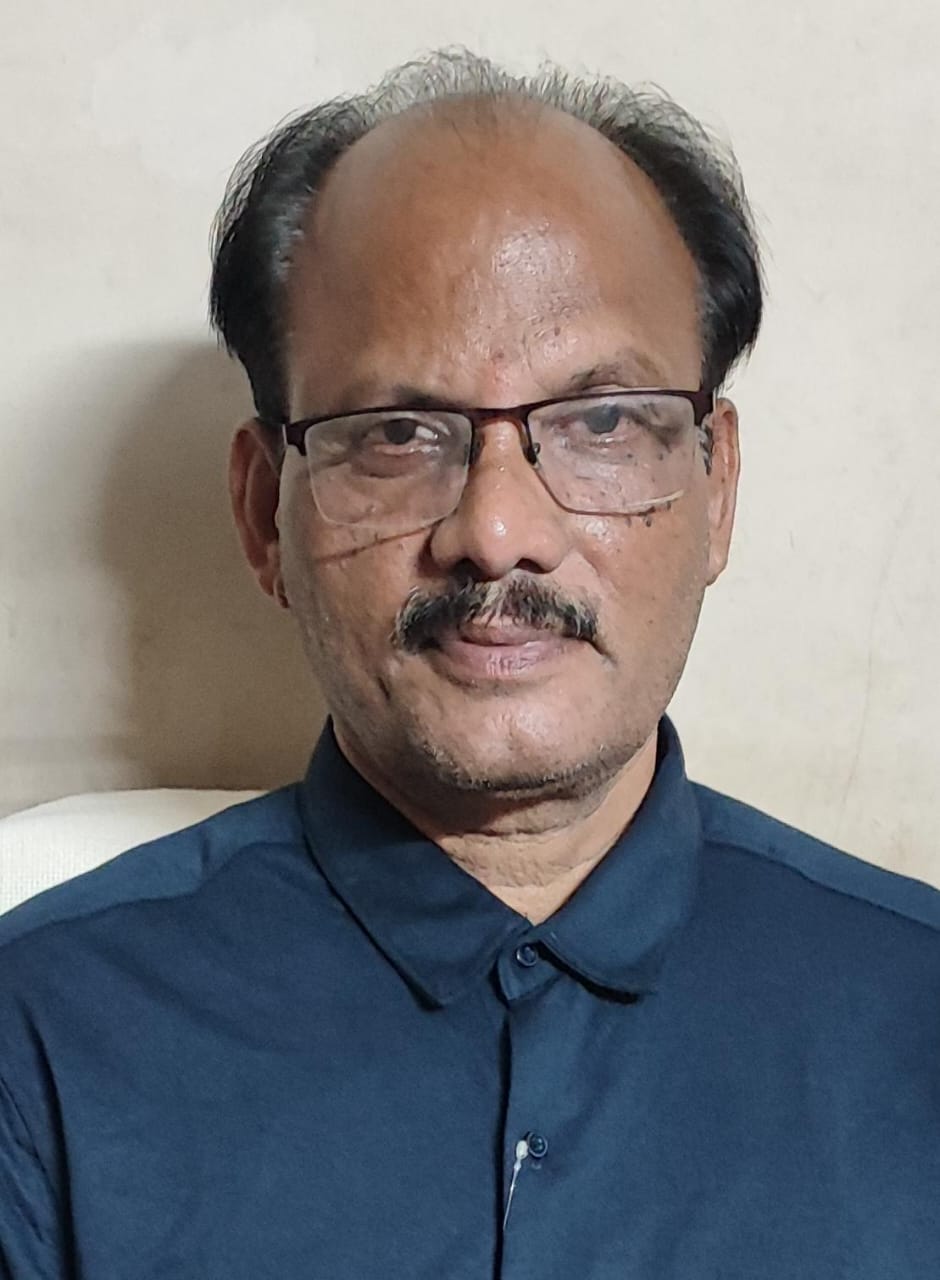

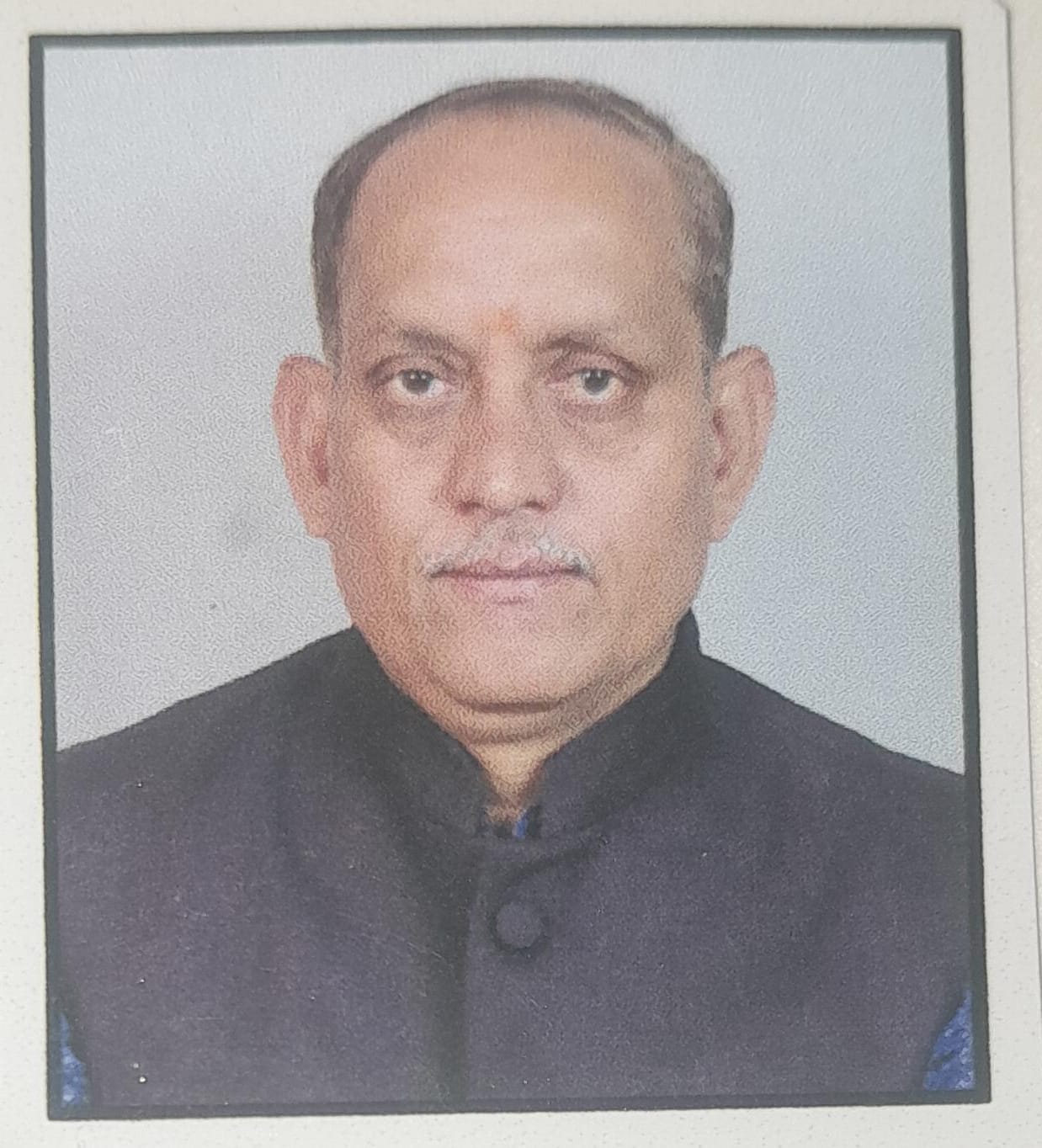
Leave a Reply