महेश अग्रवाल
पृथ्वी, पर्यावरण और मानव का गूढ़ संबंध* धरती केवल मिट्टी नहीं है,यह माँ है – हमारे अस्तित्व की जड़। हमारा शरीर पाँच तत्वों – पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश – से निर्मित है। यही तत्व प्रकृति के मूल घटक हैं। अतः जब पर्यावरण आहत होता है, तब मनुष्य का अस्तित्व स्वयं घायल होता है। किन्तु विडम्बना यह है कि जिस पृथ्वी ने हमें जीवन दिया, उसी को हमने युद्ध, प्रदूषण, लालच और विनाश की प्रयोगशाला बना दिया है। आज परमाणु बमों, रासायनिक हथियारों और औद्योगिक दुरुपयोगों ने पृथ्वी के संतुलन को गहराई से हिला दिया है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने 6 नवंबर को इस विशेष दिवस की स्थापना की – युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस – ताकि समस्त विश्व को यह स्मरण रहे कि युद्ध केवल मनुष्यों को नहीं मारता, बल्कि नदियों, वनों, पर्वतों, पशु-पक्षियों और जलवायु को भी अपंग कर देता है।
*दिवस की पृष्ठभूमि और उद्देश्य*
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2001 में यह दिवस घोषित किया ताकि युद्ध एवं संघर्ष के दौरान पर्यावरण के दुरुपयोग, प्रदूषण और विनाश के विरुद्ध विश्व चेतना जागृत की जा सके। युद्ध का प्रभाव केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, वियतनाम, और यूक्रेन जैसे उदाहरण बताते हैं कि जब बारूद जलता है, तब हवा, पानी, मिट्टी सब प्रदूषित होते हैं। विस्फोटों से निकलने वाले रासायनिक तत्व सदियों तक मिट्टी और जल में विष घोलते रहते हैं। इस दिवस का मूल संदेश है – शांति तब तक संभव नहीं जब तक प्रकृति के प्रति सम्मान न हो।
*युद्ध और पर्यावरण का विनाशकारी संबंध* युद्ध केवल सैनिकों के बीच की लड़ाई नहीं है। यह पृथ्वी के जीवन-तत्वों के विरुद्ध भी एक अस्थायी युद्ध है। रासायनिक हथियार – मिट्टी और जल स्रोतों को वर्षों तक विषाक्त बनाते हैं।परमाणु बमों के विकिरण – पीढ़ियों तक मानव-स्वास्थ्य और वनस्पति को नष्ट करते हैं। वायु प्रदूषण – कार्बन और धात्विक तत्वों से हवा को विषाक्त कर देता है। वनों की कटाई और भूमि-खनन – संसाधनों के लालच में प्रकृति को नंगा कर देते हैं।वियतनाम युद्ध में प्रयोग किए गए नारंगी एजेंट जैसे रासायनिक छिड़कावों ने लाखों हेक्टेयर जंगलों को उजाड़ दिया। कुवैत युद्ध (1991) में तेल-कुओं में लगी आग ने महीनों तक वायुमंडल को धुएँ से भर दिया। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि युद्ध का अर्थ केवल राजनीति नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी-संहार भी है।
*प्रकृति और मानव चेतना का आध्यात्मिक संबंध* भारतीय दृष्टि में प्रकृति कोई वस्तु नहीं है; वह जीवंत सत्ता है।ऋग्वेद में कहा गया – माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। यह भाव ही पर्यावरण संरक्षण का आधार है। जब तक मनुष्य स्वयं को प्रकृति का अंग मानता है, तब तक वह उसका शोषण नहीं करता। परंतु जब उसने स्वयं को प्रकृति से अलग माना, तब विनाश आरंभ हुआ। योगशास्त्र कहता है कि संसार एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है – ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं च जगत्यां जगत्। (ईशोपनिषद्) अर्थात् इस जगत में जो कुछ भी है, वह परमात्मा से ओत-प्रोत है। इसलिए किसी वृक्ष, नदी, पशु या पर्वत का विनाश, स्वयं परमात्मा के रूप का अपमान है।
*योगदृष्टि से पर्यावरण संरक्षण*
योग केवल शरीर-साधना नहीं है; यह संपूर्ण जीवन-संतुलन का विज्ञान है। पतंजलि योगसूत्र का एक सूत्र है – अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अर्थात जहाँ अहिंसा की भावना दृढ़ होती है, वहाँ वैर और हिंसा स्वतः समाप्त हो जाती है। यह अहिंसा केवल मनुष्य के प्रति नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के प्रति करुणा का भाव है। एक सच्चा योगी जब प्राणायाम करता है, तो वह केवल अपनी साँसों को नहीं, बल्कि वायुमंडल की ऊर्जा से जुड़कर पृथ्वी की जीवन-लय को अनुभव करता है। योग का प्रत्येक अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने का उपाय है।
*यम और नियम में पर्यावरण का संदेश* अहिंसा – किसी जीव या तत्व को आघात न देना। सत्य – प्राकृतिक नियमों के प्रति सत्यनिष्ठ रहना। अस्तेय – प्रकृति से अनावश्यक संसाधन न छीनना। संतोष – सीमित साधनों में सुखी रहना। ईश्वर प्राणिधान – हर तत्व में दिव्यता का अनुभव।यदि ये पाँच यम-नियम मनुष्य के व्यवहार में उतर जाएँ, तो पृथ्वी स्वयं-संतुलित हो जाएगी।
*पंचमहाभूतों की साधना और संरक्षण* योग और वेदांत दोनों मानते हैं कि शरीर और सृष्टि एक ही पंचतत्वों से बने हैं – तत्व, प्रतीक, संरक्षण का योगिक उपाय – पृथ्वी -स्थिरता, धैर्य, ध्यान, वृक्षारोपण, सतत् जीवनशैली। जल – प्रवाह, करुणा, नदियों का संरक्षण, शुद्ध जल सेवन। अग्नि – ऊर्जा, परिवर्तन, हवन, दीप, आत्मसंयम। वायु – प्राण, गतिशीलता, प्राणायाम, स्वच्छ वायु। आकाश – व्यापकता, ध्यान, मौन, आभारभाव। जब ये पाँचों तत्व शुद्ध होते हैं, तभी योगी का मन स्थिर होता है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा वास्तव में आत्म- संरक्षण का ही रूप है।
*यौगिक शांति दर्शन बनाम युद्ध संस्कृति* युद्ध की संस्कृति प्रतिस्पर्धा और अहंकार पर आधारित है। योग की संस्कृति सहयोग और समर्पण पर। युद्ध कहता है – मैं श्रेष्ठ हूँ। योग कहता है – सबमें एक ही चेतना है। यदि मानवता योगिक दृष्टि अपनाए, तो संघर्ष स्वयं मिट सकता है। क्योंकि शांति बाहर से थोपी नहीं जाती; वह भीतर से प्रस्फुटित होती है। गीता में भगवान कहते हैं – शमः दमः तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च। ये सब आंतरिक शांति के गुण हैं। जब व्यक्ति इन गुणों को विकसित करता है, तब उसका आचरण युद्ध के स्थान पर संवाद की दिशा में बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति पर्यावरण को भी शत्रु नहीं मानता, बल्कि सहयोगी तत्व के रूप में देखता है।
*हिंसा और अन्याय के बीच करुणा की साधना* सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य ने हिंसा, अत्याचार और अन्याय के दृश्य देखे हैं। युग बदलते गए, परंतु मनुष्य के भीतर की अव्यवस्था अब भी वही है। यह एक कठोर सत्य है कि समाज में आज भी हिंसा और असहिष्णुता के बीज जीवित हैं। ऐसे वातावरण में हमें निराश होने की नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता से उत्तर देने की आवश्यकता है। जहाँ हिंसा फैली हो, वहाँ करुणा की वर्षा करें,जहाँ अन्याय और अशांति का अंधकार हो, वहाँ एकता और प्रेम का दीपक जलाएँ। यही योग का सच्चा प्रयोग है – विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी अंतःशांति बनाए रखना और अपने आचरण से संसार में शांति का संचार करना। इतिहास ने प्रायः युद्धों और विजेताओं को नायक बनाया है, परंतु वास्तविक नायक तो वे हैं जिन्होंने प्रेम, करुणा और एकता का संदेश दिया – जिनमें बुद्ध, नानक और क्राइस्ट जैसे महापुरुष अग्रणी हैं। इन संतों ने सिखाया कि हिंसा का उत्तर हिंसा से नहीं, बल्कि सहनशीलता और करुणा से देना ही मानवता का धर्म है। इस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हम ऐसी शिक्षा, ऐसे आदर्शों और ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ शांति का सम्मान हो और हिंसा का बहिष्कार। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर करुणा का दीप जलाएगा, तभी एक नए युग का उदय होगा – जिसमें युद्ध, पर्यावरण-विनाश और अन्याय का अंत होगा, और मानवता योग की करुणा में पुनः खिल उठेगी।
*ध्यान, प्राणायाम और पर्यावरणीय संतुलन* प्राणायाम केवल श्वास की तकनीक नहीं, यह वायु-तत्व के प्रति श्रद्धा का अभ्यास है। जब हम सजग होकर श्वास लेते हैं, तब हम प्रकृति के प्राण से जुड़ते हैं। एक-एक श्वास यह स्मरण दिलाती है कि हवा केवल गैस नहीं, जीवन-ऊर्जा (प्राण) है। इसी प्रकार ध्यान में मनुष्य अपने भीतर और बाहर के तत्वों का संतुलन अनुभव करता है। ध्यानस्थ व्यक्ति न तो प्रकृति को भोग-वस्तु मानता है और न ही उसे त्यागता है, वह उसे ईश्वर का साक्षात् रूप मानकर पूजता है।
*जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश – तत्वों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन* भारत में प्रत्येक तत्व की पूजा की परंपरा रही है – नदी-पूजन गंगा, यमुना, नर्मदा आदि को माँ कहा गया। वृक्ष-पूजन पीपल, तुलसी, वटवृक्ष जीवनदायी प्रतीक हैं।अग्नि-पूजन यज्ञ और हवन के माध्यम से ऊर्जा का शुद्ध उपयोग। वायु-देवता प्राणवायु के रूप में पूजनीय। आकाश ब्रह्म का प्रतीक, सर्वव्यापक चेतना। यही भारतीय दृष्टि है जहाँ धर्म और पारिस्थितिकी एक-दूसरे के पूरक हैं।
*धर्म, अध्यात्म और पर्यावरण नीति* भारत में धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि कर्तव्य और संतुलन है। मनुस्मृति कहती है – धारणात् धर्म इत्याहुः – जो धारण करता है, वही धर्म है। यदि कोई नीति या व्यवहार पृथ्वी, वायु, जल और जीवन को धारण करता है, वही सच्चा धर्म है। आज की पर्यावरण नीतियाँ यदि इस अध्यात्मिक दृष्टि से प्रेरित हों, तो वे केवल कानूनी नहीं रहेंगी, बल्कि मानवीय बनेंगी। उदाहरण के लिए – ऊर्जा-नीति में सतत् विकास का विचार। औद्योगिक नीति में प्रकृति- मित्र तकनीक का प्रयोग। कृषि-नीति में ऑर्गैनिक खेती और स्थानीय संसाधन उपयोग का महत्व। जब नीति-निर्माण में आध्यात्मिक चेतना प्रवेश करती है, तो वह केवल नियम नहीं रह जाती, वह जीवन-नीति बन जाती है।
*वैश्विक प्रयास और संयुक्त राष्ट्र का दृष्टिकोण* संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन दोनों ही यह समझने लगे हैं कि पर्यावरणीय शांति, राजनीतिक शांति की पूर्वशर्त है। यूएन के 17 सतत विकास लक्ष्य में कम से कम 10 लक्ष्य सीधे-सीधे पर्यावरण और जलवायु से जुड़े हैं। इनका आध्यात्मिक सार यही है – मानवता तभी सुरक्षित है जब प्रकृति सुरक्षित है।
*भारतीय संस्कृति के उदाहरण – प्रकृति-पूजन की परंपरा* भारतीय ऋषि जानते थे कि प्रकृति के साथ संवाद ही सबसे बड़ा धर्म है। वेदों में वायु-सूक्त, आपः-सूक्त, पृथ्वी-सूक्त जैसी स्तुतियाँ प्रकृति के संरक्षण की दिव्य घोषणाएँ हैं। उपनिषदों में कहा गया – आत्मा वा अरे दृष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तव्यः। जब आत्मा की दृष्टि सबमें होती है, तो शोषण असंभव हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं – यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। अर्थात् यदि कार्य यज्ञभाव से न किया जाए, तो वह बंधन बन जाता है। इसलिए पर्यावरण के प्रति हर कार्य – वृक्षारोपण, जल-संरक्षण, स्वच्छता – यज्ञ-भावना से किया जाना चाहिए।
*व्यक्तिगत स्तर पर हमारी भूमिका* पर्यावरण-संरक्षण केवल सरकार या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की साधना है। योगिक जीवनशैली में कुछ सरल उपाय – दैनिक जीवन में अहिंसा और संयम का पालन। प्लास्टिक और रासायनिक पदार्थों से परहेज। वृक्षारोपण और जैविक खेती को प्रोत्साहन। जल-संग्रह, वर्षा-संरक्षण को जीवन-कर्तव्य बनाना। सौर-ऊर्जा, साइकिल, पैदल-चलना, योग-अभ्यास को अपनाना। जब व्यक्ति अपने भीतर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव जगाता है, तब उसका हर कदम एक ध्यान बन जाता है।
*योग और जलवायु चेतना – एक नया युगदर्शन* अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) ने यह सिद्ध किया कि योग केवल भारत का नहीं, संपूर्ण मानवता का विज्ञान है। इसी प्रकार 6 नवंबर का यह पर्यावरण-संरक्षण दिवस युद्ध और शांति दोनों की चेतना को जोड़ने वाला वैश्विक योग-दिवस बन सकता है। यदि योग-अभ्यास को विश्व- शांति- नीति से जोड़ा जाए, तो पर्यावरण योग कूटनीति का नया अध्याय खुल सकता है – जहाँ राष्ट्रों के बीच संवाद केवल राजनैतिक नहीं, बल्कि प्रकृति और प्राण-ऊर्जा के स्तर पर हो।
*योग से शांति, शांति से पर्यावरण, पर्यावरण से जीवन* पृथ्वी के संरक्षण का आरंभ मानव के भीतर की शांति से होता है। जो मनुष्य स्वयं में संतुलित नहीं, वह प्रकृति के साथ संतुलन नहीं रख सकता। अतः योग ही वह सेतु है जो मनुष्य और प्रकृति, शरीर और चेतना, राष्ट्र और विश्व – सबको जोड़ सकता है। महर्षि पतंजलि ने कहा था – योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। अर्थात् जब मन की वृत्तियाँ शांत होती हैं, तब योग होता है। जब मनुष्य के भीतर का युद्ध समाप्त होता है, तभी बाहरी युद्धों की आवश्यकता समाप्त होती है। और जब युद्ध समाप्त होता है, तभी पर्यावरण और पृथ्वी पुनः मुस्कुराने लगती है।
*अंतिम संदेश* आओ, इस 6 नवंबर को केवल एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस न मानें, बल्कि एक आध्यात्मिक संकल्प – दिवस बनाएं – जहाँ हम युद्ध की जगह संवाद चुनें, विनाश की जगह संरक्षण, और प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग। योग हमें यह सिखाता है कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह मनुष्य की आंतरिक प्रकृति है। जब यह यह शांति भीतर प्रकट होती है, तो बाहर का पर्यावरण स्वतः पवित्र, स्वच्छ और संतुलित बन जाता है। इसी में निहित है – विश्व शांति, मानवता और पर्यावरण की एकात्म चेतना।
लेखक के ये अपने विचार हैं।













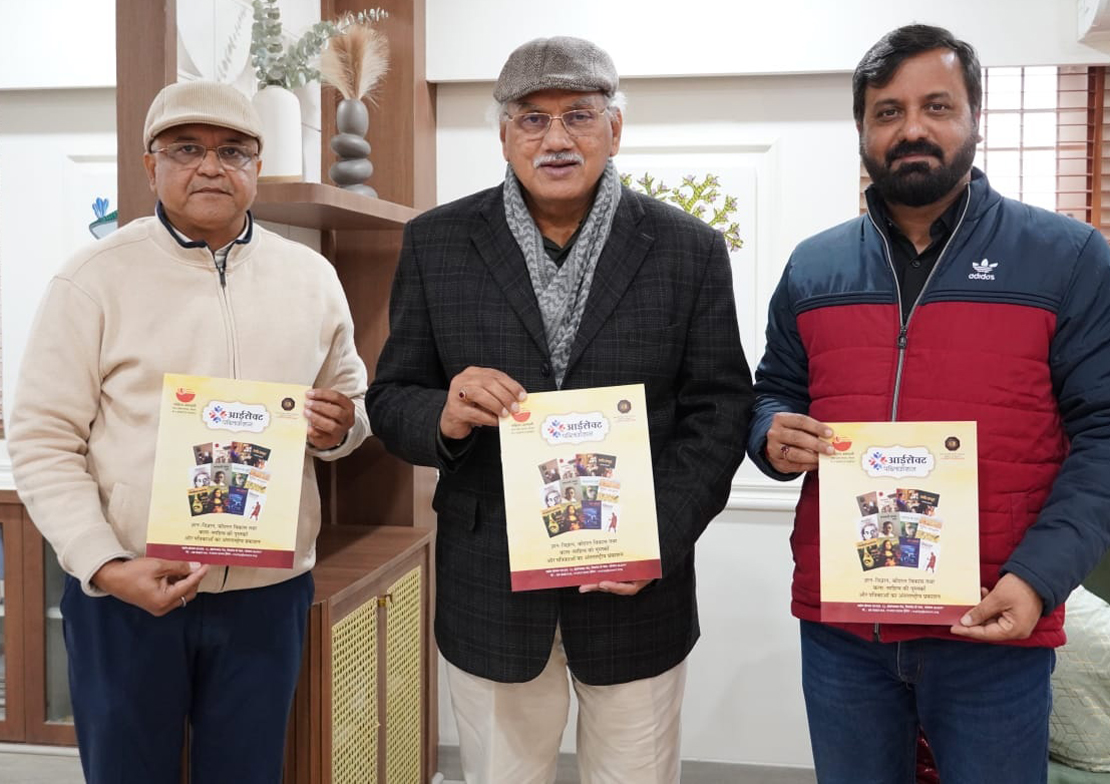



Leave a Reply