विनय उपाध्याय
मौसम और मन की प्रीत बड़ी पुरानी है। एक नया मौसम दर्द और आँसुओं को भुला देने के आग्रह के साथ, धरती पर उतरता है। जीवन के दुख भरे कि़स्से मौसम की नदी में सूखे हुए फूलों की तरह बहने लगते हैं। नया हो जाने में सुख है और आकर्षण भी। नया हो जाना हमें हल्का करता है। इसीलिए जीवन में नए पन की तलाश है।
समय निरंतर बहता हुआ सिलसिला है। इस प्रवाह की गिनती भला कैसे हो? लेकिन दिन और रात के साथ, अँधेरे और उजाले की आवाजाही को मनुष्य ने, एक इकाई मान लिया और इस तरह दिन तिथि मास और वर्ष की अवधारणा सामने आई और यूँ सतत प्रवाहित उस काल की गणना आरंभ हुई। चैत्र के इस महीने से समय को, एक नई नज़र से देखने की हमारी प्राचीन परंपरा और जीवन में नएपन को महसूस करने की हमारी एक आदिम आकांक्षा जागी।
समय की इस गिनती को अगर हम, भारतीय संदर्भों से जुड़ कर देखे, तो प्रकृति और मौसम के परिवर्तन को हमने चिन्हित किया तथा ऋतु चक्र के एक पूरे अवर्तन को, हमने वर्ष कहा। संवत्सर कहा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रीय संवत अगर कोई है तो वो है- विक्रम संवत, जिसकी 2081वीं पायदान पर हम खड़े हैं। ये अवसर है कि इस परंपरा को हम ठीक से जानें और अपने अतीत की गौरव गाथा को, बेहतर ढंग से सुने और गुने। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र प्रतिपदा, ब्रहृमा द्वारा इस सृष्टि के निर्माण की तिथि है। महाराजा विक्रमादित्य ने भारत की काल धारणा से जुड़ी सांस्कृतिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए ही चैत्र, शुक्ल प्रतिपदा की तिथि से, अपने संवत्सर, संवत की परंपरा शुरू की।
भारत के पौराणिक इतिहास पर अगर हम नज़र डालें तो भगवान श्रीराम ने लंका विजय के बाद अयोध्या में अपने राज्याभिषेक के लिए इसी प्रतिपदा के दिन को चुना। शक्ति की भक्ति के 9 दिन अर्थात चैत्र नवरात्रि का पहला दिन भी यही है। राम जन्मोत्सव ‘राम नवमी’ के पूर्व, नौ दिन उत्सव मनाने का पहला दिन। सिख परंपरा के दूसरे गुरू अंगददेव का प्रगटोत्सव दिवस भी यही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज को सद्मार्ग पर ले जाने के लिए ‘आर्य समाज’ की स्थापना इसी दिन की। सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक, वरूणावतार संत झूलेलाल भी इसी दिन प्रकट हुए। विक्रमादित्य की तरह शालिवाहन ने हूणों को परास्त कर दक्षिण भारत में श्रेष्ठतम राज्य की स्थापना इसी दिन की और महाभारत काल में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी पावन तिथि पर होता है। वसंत ऋतु में आने वाली ये तिथि चैत्र प्रतिपदा, सृष्टि के निर्माण का महान मुहूर्त है।
इस तरह इतने महान संयोगों को साथ लेकर चलती इस तिथि को अगर हमने ‘नववर्ष का शुभारंभ’ माना तो ये अत्यंत सहज और स्वाभाविक तो था ही, उपयुक्त भी था।
चैत्र मास को वैदिक काल ने मधुमास कहा। यानी आनंद लुटाता वसंत का मौसम। जब पेड़ नए पत्ते पहनने लगते हैं… फूलों पर रंग उतरने लगता है… हवा में मौसम की गमक घुलने लगती है… आम्र मंजरियाँ, तोरन द्वार सी सज उठती हैं… ये सब रूह और मन को रंगने लगते हैं…। एक नया राग बज उठता है। प्रकृति के इस विराट आयोजन को ही हम ‘नव वर्ष’ कह सकते हैं।
मौसम और मन की प्रीत बड़ी पुरानी है। एक नया मौसम दर्द और आँसुओं को भुला देने के आग्रह के साथ, धरती पर उतरता है। जीवन के दुख भरे कि़स्से मौसम की नदी में सूखे हुए फूलों की तरह बहने लगते हैं। नया हो जाने में सुख है और आकर्षण भी। नया हो जाना हमें हल्का करता है। इसीलिए जीवन में नए पन की तलाश है।
प्रसंगवश उस नायक की छवि कौंधती है जिसने भारत की सांस्कृतिक अस्मिता और उसके गौरव का मान रखते हुए उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के लिए आखिरी साँस तक अपनी आस्थाओं का अभिषेक किया। इस अदम्य पुरूषार्थी को इतिहास महाराजा विक्रमादित्य के नाम से जानता-पहचानता है।
वे ही नव सम्वत्सर के प्रणेता हैं। इधर मध्यप्रदेश के संस्कृति महकमे के अधीन संचालित स्वराज संस्थान संचालनालय की महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ ने अध्ययन, चिंतन और शोध की नई दिशाएँ तय करते हुए विक्रमादित्य के जीवन के अनेक अज्ञात, अनछुए और अलक्षित पहलुओं तथा इस तारतम्य में भारतीय इतिहास को सहेजने का कार्य किया है। सक्रियता के इस विस्तार में कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है। विचार संगोष्ठियों और सांस्कृतिक गतिविधियों के ज़रिये विक्रमादित्य के विलक्षण योगदान से जन-मानस को परिचित कराने का अभियान भी आरंभ हुआ है। इन दिनों शोध पीठ के मुख्यालय उज्जैन (जो विक्रमादित्य की कर्मभूमि रहा है) का रंगमंच ‘विक्रमोत्सव’ से गुलज़ार है। एक नई दृष्टि इतिहास पुरूष के आसपास खुल रही है। विमर्श के नए छोर भी हाथ लग रहे हैं। सांस्कृतिक हस्तक्षेप का नया परिवेश निर्मित हो रहा है।
स्वाधीन भारत में संविधान स्वीकार करते समय राष्ट्र गान एवं राष्ट्र ध्वज के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर दो सम्वत् अंगीकार किये गये है। पहला ईस्वी सम्वत् और दूसरा शक सम्वत् ये दोनों ही सम्वत् भारत आक्रांताओं और उसे पराधीन बनाने वाली शक्तियों द्वारा प्रवर्तित किये गये हैं। जहाँ तक ईसवी सम्वत् का प्रश्न है यह एक तरह से इसकी अंतराष्ट्रीय स्वीकृति की वजह से मान्य किये जाने योग्य है, परन्तु शक सम्वत् को भी राष्ट्रीय स्तर पर मान्य कर लिया जाना आपत्तिजनक है।
भारतीय संस्कृति पर अभिमान करने वालों के लिए यह निश्चय ही गौरव का विषय है कि आज भारत वर्ष में प्रवर्तित विक्रम सम्वत्सर बुद्धनिर्वाणकाल गणना को छोड़ कर संसार के प्रायः सभी ऐतिहासिक सम्वतों में प्राचीन है। यह भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। विक्रम संवत् के उद्भव तक विशुद्ध वैदिक संस्कृति का काल, रामायण और महाभारत का युग, महावीर, गौतम बुद्ध का समय, चंद्रगुप्त मौर्य एवं प्रियदर्शी अशोक, पुष्यमित्र व शुंग की साहसगाथा, वेद, पुराण, सूत्रग्रंथ एवं स्मृतियों की रचना भारतवर्ष में हो चुकी थी। पाणिनी, पतंजलि और चाणक्य का पांडित्य तथा राजनीतिक बुद्धिमत्ता चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। विक्रमादित्य का समय भारशिवनागों, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, यशोवर्मन, विष्णुवर्द्धन के बल और प्रताप की चमक से विश्व को चमत्कृत करने का समय था। यह ही वह समय था जब दुनिया के कई भागों में भारत की संस्कृति व धर्म की सुगंध फैल रही थी। कालिदास, भवभूति, भारवि, भतृहरि, वराहमिहिर, माद्य, दंडी, बाणभट्ट, धन्वतरि, कुमारिल भट्ट, नागार्जुन आदि की प्रतिभा पर सारी दुनिया मुग्ध थी।
ग़ौर करने की बात ये भी कि विक्रम सम्वत् का प्रवर्तन विक्रमादित्य द्वारा उज्जैन से किया गया। उज्जैन परम्परा से ही काल गणना का एक प्रमुख केन्द्र माना जाता रहा और इसीलिए अरब देशों में भी उज्जैन को ‘अजिन’ कहा जाता रहा। सभी ज्योतिष सिद्धांत ग्रंथों में उज्जैन को मानक माना गया है। आज जो वैश्विक समय के लिए ग्रीनविच की स्थिति है वह ज्योतिष के सिद्धांत काल में और उसके बाद सैकड़ों वर्षों तक उज्जैन की रही। यह भी निर्विवाद है कि ज्योतिर्विज्ञान उज्जैन से यूनान और एलेक्जेंड्रिया पहुँचा। काल गणना केन्द्र होने से उज्जैन को विश्व के नाभि स्थल की मान्यता भी रही है। यह गणना महाकालेश्वर के उज्जैन में होने के काल विशेष के संदर्भ से भी जुड़ती है। इस प्रकार विक्रम सम्वत् ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार भी एक विशेष महत्व रखता है।
विदेशियों द्वारा शुरू किये गये सम्वत् को भारत में स्वीकार किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर सटीक राष्ट्र कैलेंडर अंगीकार करने के लिए गठित समिति की वर्ष 1955 में प्रकाशित रिपोर्ट की भूमिका में पं. जवाहर लाल नेहरू ने लिखा कि- “विभिन्न कैलेंडर देश में पिछले राजनीतिक विभाजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है तब यह वांछनीय है कि कैलेंडर में हमारी नागरिक, सामाजिक और अन्य आवश्यकताओं की एकरूपता हो और इस समस्या का निदान वैज्ञानिक आधार पर हो।” लेकिन राजनैतिक खानाबंदियों के चलते ऐसा हो न सका। भारत की राष्ट्रीयता, सामाजिकता, उसकी उत्सवधर्मी संस्कृति और वैज्ञानिक आधारों को दरकिनार करते हुए समय की गणना का पश्चिमी मानक देश की जनता पर थोप दिया गया।
ऋषि परंपरा कहती है- “जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है। पुष्प देता है, संवेदना देता है और हमें दया भाव सिखाता है उसी तरह यह नव वर्ष हमें हर पल ज्ञान दे। हमारा हर दिन मंगलमय हो!”














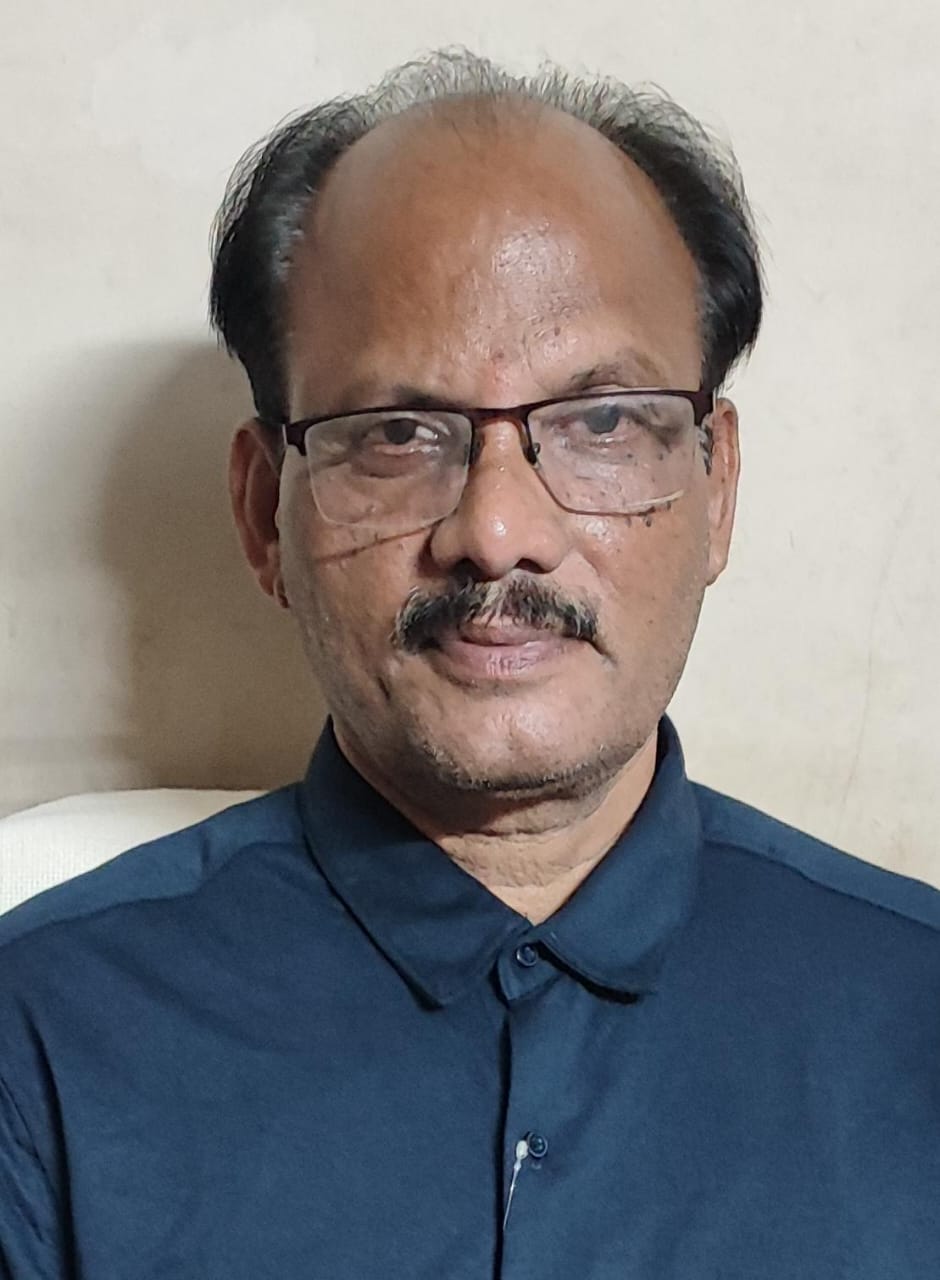

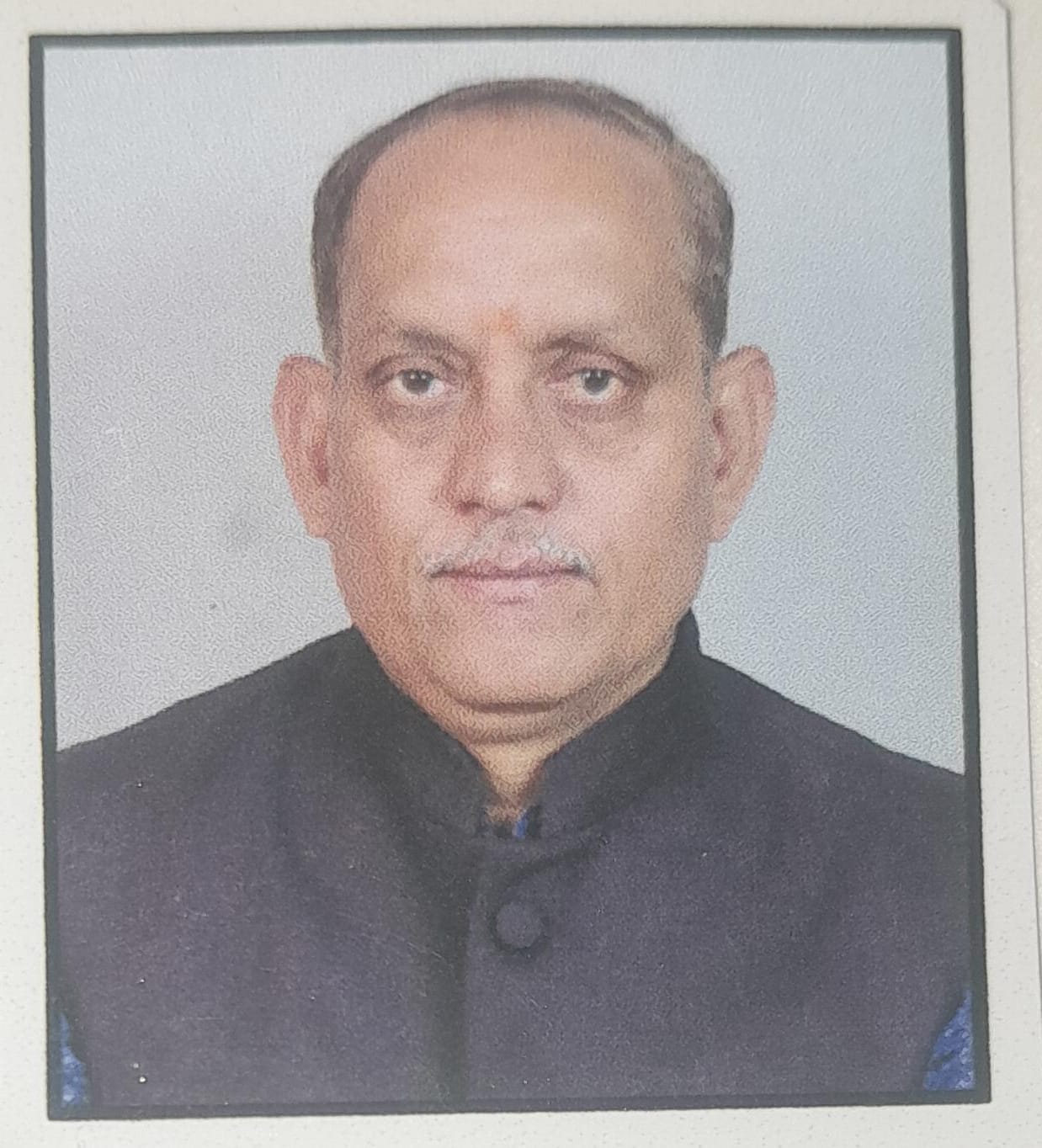
Leave a Reply