भोपाल। आदर्श योग आध्यात्मिक केंद्र स्वर्ण जयंती पार्क कोलार रोड़ भोपाल के योग गुरु महेश अग्रवाल ने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों के मूलभूत अधिकारों की सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। आदिवासी शब्द दो शब्दों ‘आदि’ और ‘वासी’ से मिल कर बना है और इसका अर्थ मूल निवासी होता है। पुरातन संस्कृत ग्रंथों में आदिवासियों को अत्विका’ नाम से संबोधित किया गया एवं भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति पद का उपयोग किया गया है। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के निम्न आधार हैं- आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक पृथक्करण, समाज के एक बड़े भाग से संपर्क में संकोच या पिछड़ापन। आदिवासियों की देशज ज्ञान परंपरा काफी समृद्ध है।
किसी भी जाति की पहचान समाज में उसके विशिष्ट कार्यों से होती है, कार्य ही व्यक्ति, जाति, जनजाति को समाज में प्रतिष्ठा प्रदान करता है। सोने का काम करने वाला सोनार, लोहे का कार्य करने वाला लोहार, मछली पकड़ने वाला मछुवारा नाव चलाने वाला नाविक आदि इसके कार्यों से इनकी पहचान है। किन्तु ये कैसी अजीव है कि वनस्पति की विभिन्न जड़ी बूटियों की कुशल जानकारी रखने वाला उन जड़ी बूटी की पहचान कर घने जंगलों से तोड़कर लाने वाला आर्थिक शोषण का जबरदस्त शिकार है।
योग गुरु अग्रवाल ने बताया कि “आदिवासी जीवनशैली में योग, धर्म और आध्यात्मिकता का स्वाभाविक समावेश” आदिवासी समाज, जिसे अक्सर “वनवासी” या “जनजातीय समुदाय” कहा जाता है, आधुनिकता की चकाचौंध से दूर, प्रकृति के सान्निध्य में जीवन यापन करता है। उनका जीवन सरल, स्वाभाविक और संतुलित होता है। यद्यपि उन्होंने “योग”, “धर्म” या “आध्यात्मिकता” जैसे शब्दों को कभी औपचारिक रूप में नहीं अपनाया, फिर भी उनका सम्पूर्ण जीवन इन तत्वों की मूर्त अभिव्यक्ति रहा है। आदिवासी जीवन और योग का गहन संबंध: प्राकृतिक जीवनशैली ही योग है:आदिवासी समाज दिनचर्या को सूर्य के उदय और अस्त से जोड़ते हैं, जो योग की “सूर्य नमस्कार” और “प्राकृतिक ऋतुचक्र के अनुसार जीवन” की परंपरा से मेल खाती है। शारीरिक श्रम और आसनों की समानता : जंगलों में चलना, लकड़ी काटना, पानी भरकर लाना, कृषि करना – ये सभी कार्य शरीर को लचीलापन, संतुलन और बल प्रदान करते हैं। यह सब सहज योग का ही रूप है। प्राणायाम जैसी सांस की तकनीक:जंगलों की शुद्ध हवा में रहने के कारण उनका श्वसन स्वाभाविक रूप से गहरा और संतुलित होता है, जो प्राणायाम की आत्मा है।
आदिवासी धर्म, लोक परंपराएँ और देवता – ईश्वर से सीधा संवाद आदिवासी धर्म का मूल भाव किसी बाहरी माध्यम, ग्रंथ या पंडित पर आधारित नहीं होता – यह प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष संवाद का धर्म है। उनके लिए पेड़, नदियाँ, चट्टानें, अग्नि और आकाश केवल प्राकृतिक तत्व नहीं, बल्कि पूज्य देवता हैं। यह सीधा संबंध ही सच्चे अध्यात्म का रूप है – जहाँ प्रकृति पूजा के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर से आत्मिक रूप से जुड़ता है। यह भावना सनातन धर्म के मूल मंत्र “सर्वे भवन्तु सुखिनः” की सजीव अभिव्यक्ति है, जहाँ समस्त सृष्टि के कल्याण की कामना निहित है। त्योहार और उपासना: ऋतु, राग और श्रद्धा की अभिव्यक्ति आदिवासी पर्व जैसे सरहुल, कर्मा, और भौमिका – सभी प्रकृति, ऋतुओं और कृषि चक्र से गहराई से जुड़े होते हैं।
इन त्योहारों में नृत्य, संगीत, सामूहिक भजन और वादन प्रमुख होते हैं – जो धर्म को केवल पूजन की प्रक्रिया नहीं, जीवन की उत्सवधर्मिता बनाते हैं। देवता: धरती से आकाश तक फैला ईश्वरत्व उनके प्रमुख पूज्य हैं —धरती माता, जलदेवता, वनदेव, सूर्य और चंद्र, कुल देवी-देवता तथा पूर्वजों की आत्माएँ। यह श्रद्धा किसी मूर्ति या मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि जीवंत प्रकृति में निवास करती है।
मार्गदर्शक: गुरु नहीं, अनुभव है आदिवासी समाज में कोई बाहरी गुरु आवश्यक नहीं होता। प्रकृति स्वयं शिक्षक है और अनुभवी वृद्धजन जीवन की राह दिखाते हैं। यह मार्गदर्शन शुद्ध लोकधर्म का परिचायक है — जिसमें कर्मकांड की जटिलता नहीं, केवल श्रद्धा, अनुभव और सामूहिक चेतना होती है।
आदिवासी धर्म हमें सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए बाहरी साधनों की नहीं, भीतर की सरलता और प्रकृति के प्रति आभार की आवश्यकता है। उनकी धार्मिकता, पूजा और उपासना में योग, भक्ति और अध्यात्म का सहज संगम है — जो आज की दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है। आदिवासी जीवन में आध्यात्मिक चेतना: सामूहिकता में आत्मा का अनुभव:आदिवासी समुदाय “मैं” नहीं, “हम” में विश्वास रखता है। यह ‘अहंकार विहीन’ सामूहिकता ही गहरी आध्यात्मिक अनुभूति की नींव है। त्याग और संतुलन:वे जंगल से उतना ही लेते हैं जितना ज़रूरत हो, कभी संग्रह नहीं करते। यह योग और अध्यात्म की ‘अपरिग्रह’ की भावना का श्रेष्ठ उदाहरण है। आत्मा का सम्मान:वे मानते हैं कि हर पेड़, नदी, पत्थर में आत्मा है। यह वेदों की “ईशावास्यमिदं सर्वं” की उद्घोषणा का सजीव रूप है।
आदिवासी लोककला, हस्तशिल्प और अध्यात्म: मांडना, वर्ली, गोंड चित्रकला केवल कला नहीं – ध्यान, साधना और शक्ति के प्रतीक हैं। ये चित्र ब्रह्मांड की संरचना, देवता, जीवों और प्रकृति के बीच संतुलन को दर्शाते हैं। यह ध्यान और चित्त की एकाग्रता का अभ्यास है। लोकगीत और मंत्र: उनके गीतों में आध्यात्मिक भाव, सृष्टि की रचना और जीवन के गहरे तत्वों की अभिव्यक्ति होती है। ये गीत अनायास ध्यान की स्थिति उत्पन्न करते हैं।
आज के समाज के लिए संदेश: यदि हमें जीवन में शांति, संतुलन और सत्य चाहिए – तो हमें आदिवासी समाज से सीखना होगा कि योग केवल शरीर की कसरत नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक सहज कला है। धर्म कोई अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सौहार्द है। और अध्यात्म कोई प्रवचन नहीं, बल्कि ‘प्रकृति से तादात्म्य’ की सच्ची अनुभूति है।
आदिवासी समाज किसी पंथ, जाति या परंपरा से नहीं, बल्कि मानवता और प्रकृति के सनातन संबंध से बंधा है। वे हमें सिखाते हैं कि योग, धर्म और अध्यात्म – ये कोई पढ़ने की चीज़ें नहीं, बल्कि जीने की विधा है। उन्हें समझना ही सच्चे योग की ओर पहला कदम है। आदिवासी संस्कृति का सम्मान करें, उनसे सीखें, और अपनी जीवनशैली को सरल, संतुलित और आध्यात्मिक बनाएं – यही आज की सच्ची आवश्यकता है।
भारत की सांस्कृतिक जड़ें जितनी गहरी हैं, उतनी ही प्राचीन और दिव्य उसकी आदिवासी परंपराएँ भी हैं। आदिवासी समाज कोई पिछड़ा वर्ग नहीं, बल्कि वह मूल चेतना है जिसने प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व, योग, अध्यात्म और धार्मिक अनुशासन को सहज जीवनशैली के रूप में अपनाया है।
आदिवासी जीवन और योग का संबंध – योग एक क्रिया नहीं, जीवन है – जिसे आदिवासियों ने जिया है। आदिवासी समाज में शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बचपन से ही जीवनशैली का हिस्सा होता है। दैनिक जीवन में उनका चलना, उठना, बैठना, श्वास की लय, पेड़ों से संवाद और नृत्य – सब योग के अंग हैं। वृक्षासन, ताड़ासन, पद्मासन, नटराज मुद्रा जैसी कई योगमुद्राएँ उनकी परंपरागत नृत्य मुद्राओं में स्वतः समाहित हैं। वे प्राकृतिक ध्यान करते हैं – बहते झरनों, पत्तों की सरसराहट, अग्नि की लौ और चंद्रमा की शीतलता में।
अध्यात्म: प्रकृति के साथ आत्मा का संवाद – “प्रकृति ही उनका मंदिर है, और जीवन ही साधना।” आदिवासी अध्यात्म बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अंतःचेतना और अनुभव से जुड़ा होता है। वे पेड़ों, नदियों, पर्वतों, अग्नि और आकाश को देवता रूप में पूजते हैं – यह संपूर्ण सृष्टि के प्रति भक्ति है। उनका हर कर्म – चाहे बीज बोना हो या शिकार करना – एक आध्यात्मिक संकल्प होता है, जो ब्रह्मांडीय नियमों के अनुरूप होता है। वे एकता, सहयोग, संतोष और संतुलन को सर्वोच्च आध्यात्मिक मूल्य मानते हैं।
जीवनशैली: योग, अध्यात्म और धर्म का जीता-जागता स्वरूप सादा जीवन, उच्च विचार – यही उनका धर्म है। भोजन सात्विक, मौसमी और सामूहिक होता है – जिसमें अहिंसा, संतुलन और शुद्धता की भावना होती है। प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना, जल का संरक्षण, वृक्षारोपण, जन सहयोग, संगीत, साप्ताहिक उपवास – यह सब योगिक अनुशासन का अंग है। पर्यावरण के साथ पूर्ण समरसता, स्त्री-पुरुष की समान भूमिका, समाज में कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं – यह सब अध्यात्म की ऊँचाई दर्शाते हैं।
आदिवासी समाज कोई पिछड़ा नहीं, बल्कि वह प्राचीन ऋषि परंपरा का जीवित स्वरूप है। उनका जीवन स्वयं में एक योगशास्त्र, अध्यात्मविज्ञान और धर्मग्रंथ है – जिसे शब्दों में नहीं, अनुभव और सम्मान से समझा जा सकता है। आज जब हम आधुनिक जीवन में भटकते हुए योग और अध्यात्म को खोज रहे हैं, तब हमें आदिवासी समाज से सीख लेनी चाहिए कि कैसे बिना किसी दिखावे, बिना किसी प्रचार के, साधारण जीवन जीते हुए भी एक श्रेष्ठ आत्मिक जीवन जिया जा सकता है। वंदन उन आदिवासी ऋषियों को जिन्होंने हमें प्रकृति, योग और धर्म की सच्ची राह दिखाई। जय प्रकृति, जय योग, जय मानवता।
योग गुरु अग्रवाल ने बताया क्या योग दुनिया की गरीबी की समस्या का समाधान कर सकता है? अगर हर आदमी गरीबी चाहने लगे तो संसार स्वर्ग बन जायेगा। लेकिन यहाँ तो हर कोई अमीर बनने की कोशिश में जी-जान से लगा हुआ है। सभी कालों में, सभी देशों के सन्तों ने कहा है कि सच्चे व्यक्ति का जीवन आत्म स्वीकृत गरीबी से भरा जीवन होना चाहिये। वस्तुतः निर्धनता शब्द को सरलता में बदल देना चाहिये। जीवन में सरलता का मतलब हुआ- अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं और सीमित सुविधाओं के हिसाब से जीवन निर्वाह करना। अपनी भौतिक जरूरतों को बढ़ाते ही हम अपने आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन स्तर में अनेक जटिलताएँ पैदा कर लेते है। कहा गया है कि एक ऊँट का सुई के छेद से निकल जाना आसान है, लेकिन एक धनवान आदमी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाना कठिन है। व्यक्ति जब धनवान बन जाता है तब उसका दिमाग निष्क्रिय हो जाता है। दौलत इंसान के लिये अफीम है। इसलिये सीमित आवश्यकताओं में जिन्दगी बिताने की भरपूर कोशिश करनी चाहिये। आजकल अधिकतर देश गरीबी दूर करने का कठिन प्रयत्न कर रहे हैं। वे अपनी जनता का जीवन-स्तर ऊपर उठाने में लगे हैं। लेकिन सारी प्रक्रिया को उलट देना चाहिये, वापस चलो- गरीबी, सरलता और प्राकृतिक जीवन की ओर।





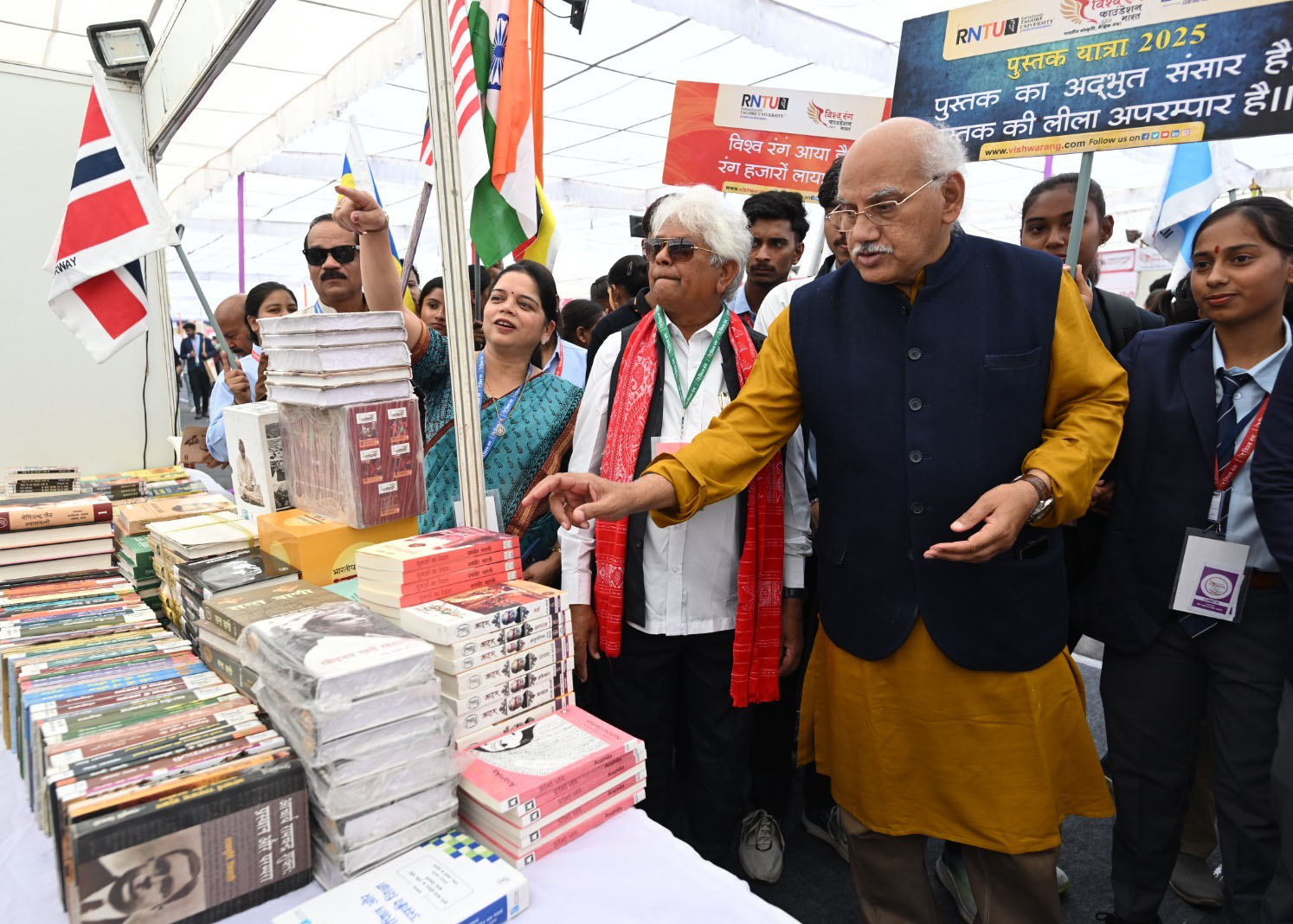
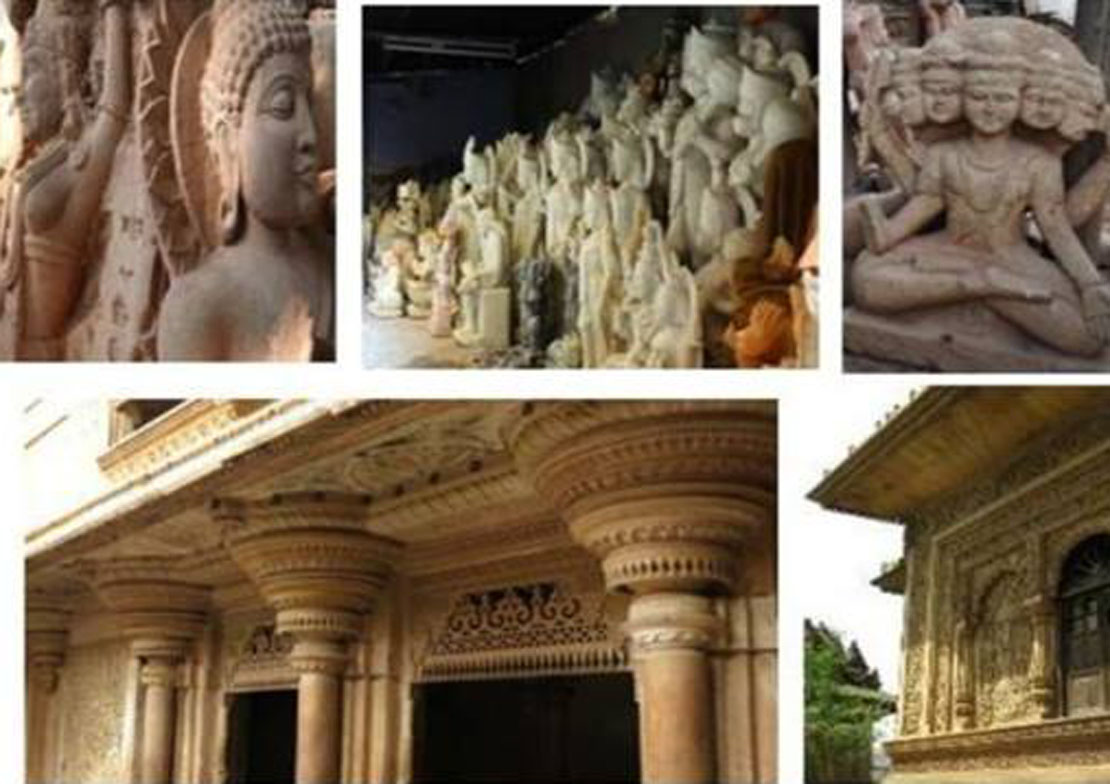









Leave a Reply