राधेश्याम रघुवंशी
दुनिया भर में प्रकृति को बचाने हेतु प्रयासों की चर्चा तो होती है परंतु धरातल पर उसके परिणाम नजर नहीं दिखते। प्रकृति को ध्यान में रखकर योजना बनाना चाहिए यह सभी देश जानते है परंतु सकारात्मक परिणामों के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों को आकर्षक और बहु-कार्यात्मक बनाना चाहिए। प्रकृति-आधारित समाधानों को डिजाइन करने के लिए डिजाइनरों, कलाकारों और वास्तुकारों के साथ सह-निर्माण करना चाहिए। प्रकृति पथ बनाते समय पानी को ध्यान में रखना चाहिए। विकास कार्यों की योजना बनाते समय प्रकृति के नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रकृति को बचाने के लिए वायु, जल, और भूमि प्रदूषण को कम करना चाहिए। पेड़-पौधों का संरक्षण करने के लिए वृक्षारोपण अभियानों में भाग लेना चाहिए । वन्यजीवों के संरक्षण के लिए योगदान करना चाहिए। पानी की खपत कम करनी चाहिए। प्रकृति के प्रति नैतिक और आचारिक चिंता विकसित करके करुणा दिखाई जा सकती है. इसके लिए नैतिक उत्पादों का चयन करना या वन्यजीवों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करना चाहिए। विकास कार्यो की योजना बनाते समय प्रकृति के नियमों को ध्यान में रखने की जरूरत ठाकरे प्रकृति के नियमों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यो की योजना बनाने की आवश्यकता है। विश्व पर्यावरण कल्याण के लिए भारतीय संस्कृति पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। विकास कार्यों की योजना बनाते समय हमें प्रकृति के नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के परिणामों को देखा हैं। हम पृथ्वी को वसुंधरा कहते हैं और उसकी तुलना वर्ग फुट के माप से करते हैं और इसे विकास कार्यो की योजना बनाते समय प्रकृति के नियमों को ध्यान में रखने की जरूरत है।
कोरोना वायरस के कारण, अब हम आक्सीजन के महत्व को महसूस कर रहे हैं और अब आक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को उन्नत कर रहे हैं। लेकिन पेड़ों की तरह प्राकृतिक रूप से मिलने वाली आक्सीजन नष्ट हो रही है। बढ़ते प्रदूषण और जल संकट जैसी समस्याओं से जूझ रहा है देश भारत जो सबसे निचले पायदान पर है, वो वायु गुणवत्ता में आती गिरावट, तेजी से बढ़ता उत्सर्जन, भूजल में गिरावट, प्रदूषण और पानी की कमी से सूखती नदियां और जल स्रोतों के साथ हर जगह लगते कचरे के पहाड़ जैसी पर्यावरण सम्बन्धी अनगिनत चुनौतियों से जूझ रहा है। इतना ही नहीं ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे संवेदनशील देशों में से भी भारत एक है। इसमें कोई दोराय नहीं की आज हमारा देश भारी जल संकट का सामना कर रहा है, हमारे 70 फीसदी भूजल स्त्रोत सूख चुके हैं। वहीं इनके पुनर्भरण की दर 10 फीसदी से भी कम रह गई है। चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहर पहले ही पानी की कमी को लेकर सुर्खियों में हैं। वायु गुणवत्ता का आलम यह यह कि स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी संगठन आईक्यू एयर ने अपनी रिपोर्ट में भारत को 2023 का तीसरा सबसे प्रदूषित देश घोषित किया है। विडम्बना देखिए कि दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 42 भारत में हैं। हैरानी की बात है कि पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर आती गिरावट के बावजूद देश में पर्यावरण और प्राकृतिक प्रणालियों की रक्षा के लिए बनाए कई कानून पिछले कुछ वर्षों में बदलावों के चलते कमजोर हुए हैं। हालांकि इसको लेकर व्यापक तौर पर जन विरोध भी हुए हैं। उत्तर में हिमालय और अरावली में हमारे जल, जंगल, नदियां, पहाड़ और रेगिस्तान इंसानी प्रभावों के चलते गिरावट का सामना कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ भारत के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिला है, इनमें हसदेव वन क्षेत्र शामिल हैं। वहीं निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी घाट में पुरातन वर्षावनों का बड़े पैमाने पर दोहन किया गया है। इन क्षेत्रों में बांध परियोजनाओं के साथ-साथ बड़े स्तर की अन्य संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसी तरह कोयला, पत्थर और रेत खनन ने इन क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर दोहन किया है। देश के विभिन्न राजनीतिक दलों व नेताओं को पर्यावरण को बचाने हेतु उचित प्रयास करना चाहिए। हमारी प्राकृतिक और लोकतांत्रिक विरासत की सुरक्षा के लिए नई प्रतिबद्धता और संवाद जरूरी है। भारत में विकास की परिभाषा में बदलावों की बात भी करी है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर विकास नहीं होना चाहिए। इससे प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हमारे प्राकृतिक प्रणाली का विनाश हो रहा है। वहीं पानी का गहराता संकट हमारे युवाओं और वन्यजीवों के भविष्य के लिए खतरा बन रहा है, जिससे निपटना जरूरी है। हिमालय, अरावली, पश्चिमी और पूर्वी घाटों, तटीय क्षेत्रों, आर्द्रभूमियों, नदी घाटियों, मध्य भारतीय और उत्तर-पूर्वी वन क्षेत्रों में पारिस्थितिक तंत्र और सामुदायिक आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक क्षेत्रों में कार्पोरेट शोषण पर रोक लगाने पर जोर दिया है। स्थानीय और राष्ट्रीय विकास से जुड़ी सभी निर्णय प्रक्रियाओं में समुदाय और नागरिक समाज को मुख्य रूप में शामिल करने पर जोर दिया जाना चाहिए। प्रकृति और उस पर निर्भर समुदाय के अधिकारों के साथ-साथ हमारी भावी पीढ़ियों के अधिकारों को सभी विकास योजनाओं के मूल सिद्धांत के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए। ग्राम सभा की सहमति के बिना वन व कृषि भूमि में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। पर्यावरण एवं प्रकृति के संरक्षण के लिए कई संगठनों ने मांग की है कि 2014 के बाद से पर्यावरण और वन अधिनियमों को कमजोर करने वाले सभी प्रावधानों को बदला जाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता अधिनियम, वन अधिकार कानून, के साथ प्रकृति और मूल निवासियों के अधिकारों को बनाए रखने वाले सभी कानूनों का पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
भारत में सूख चुकी सभी नदियों, जोहड़ों, झीलों, तालाबों और अन्य जल निकायों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। साथ ही हमारे देश की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके जल पुनर्भरण के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाना चाहिए। हिमालय, अरावली और पश्चिमी घाटों में नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं, बांध निर्माण, सुरंग बनाने के लिए किए जाने वाले विस्फोटों और हमारे पहाड़ों को काटने वाली सभी परियोजनाओं पर रोक लगाईं जानी चाहिए और इन परियोजनाओं को शुरू करने से पहले उनके प्रभावों का मूल्यांकन करने और इनके लिए आम लोगों की राय ली जानी चाहिए।
संपूर्ण भारत में शहरीकरण, बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं और व्यवसायीकरण के लिए भूमि उपयोग में बदलाव से पहले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट आपदा और क्लाइमेट रिस्क अध्ययन को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इसी तरह पहाड़ों पर होते खनन को रोकने के लिए निर्माण गतिविधियों में सतत और वैकल्पिक निर्माण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीतियों का तत्काल कार्यान्वयन होना चाहिए। इसी तरह जंगल और आवास क्षेत्रों के आसपास होने वाली सभी खनन गतिविधियों को रोका जाना चाहिए। ताकि इसके लिए किए जाने वाले विस्फोट और खनन गतिविधियों के चलते स्थानीय समुदायों और वन्यजीवों के स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े और वो सभी शांति से रह सके। इसी तरह प्राकृतिक पारिस्थिति के तंत्र को हमारी भावी पीढ़ियों के लिए संजोया जा सके।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए। सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सीवेज और अपशिष्ट जल के सुरक्षित उपचार, पुनर्चक्रण और निर्वहन के लिए एसटीपी और ईटीपी स्थापित किए जाने चाहिए। हम भारतीयों को यह नहीं भूलना चाहिए कि वास्तव में सुशासन, नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जन प्रतिनिधियों के साथ-साथ नागरिकों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। सबके साथ से ही देश एक बेहतर कल और सतत एवं न्यायसंगत विकास की राह में आगे बढ़ सकता है। मतदान सिर्फ राजनैतिक दलों और नेताओं का महज चयन ही नहीं यह प्रकृति की सुरक्षा, बेहतर कल, सभी नागरिकों के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी और भारत के युवाओं के लिए एक सुरक्षित भविष्य की कुंजी भी है।
लेखक के ये अपने विचार हैं।














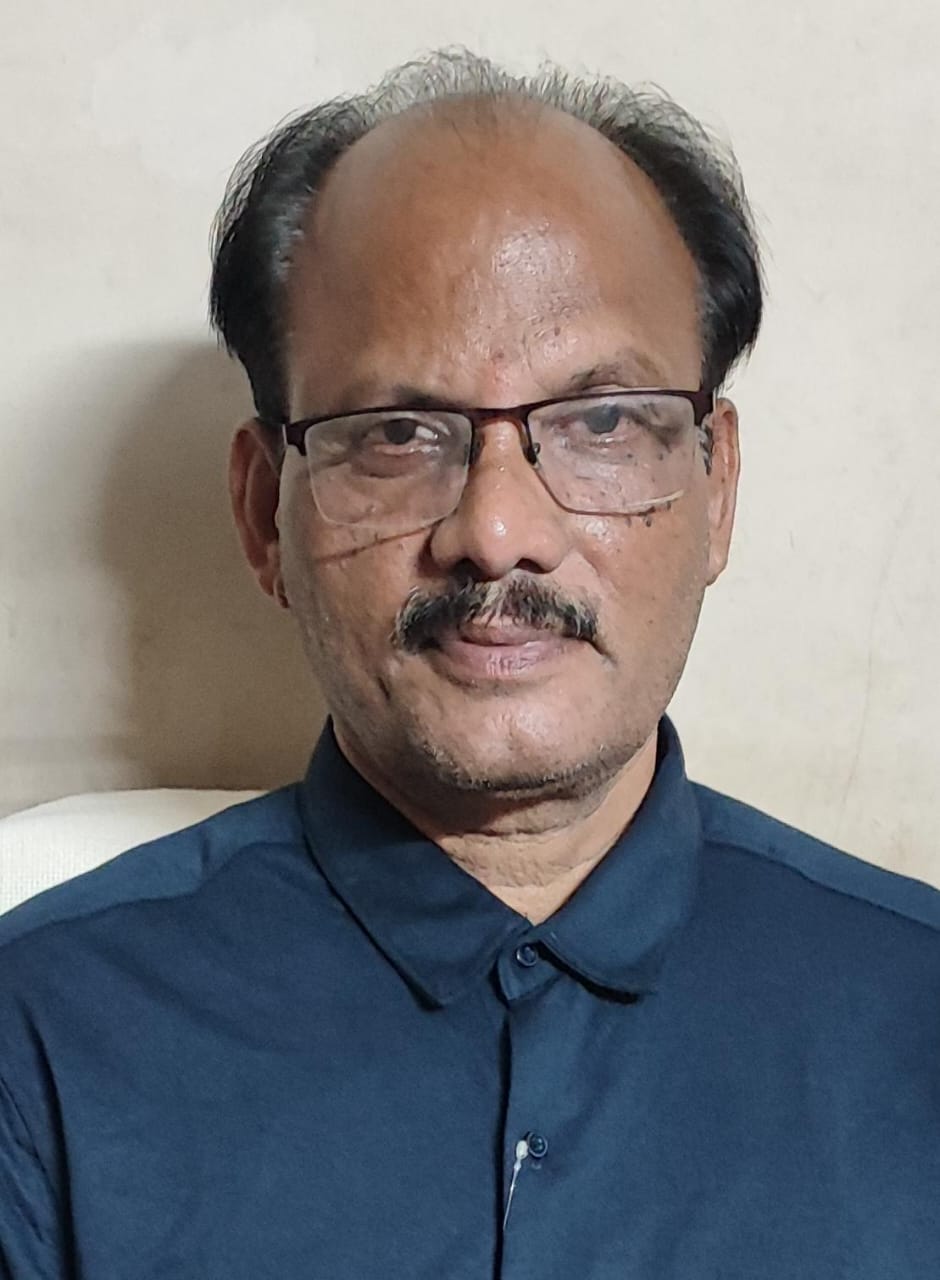

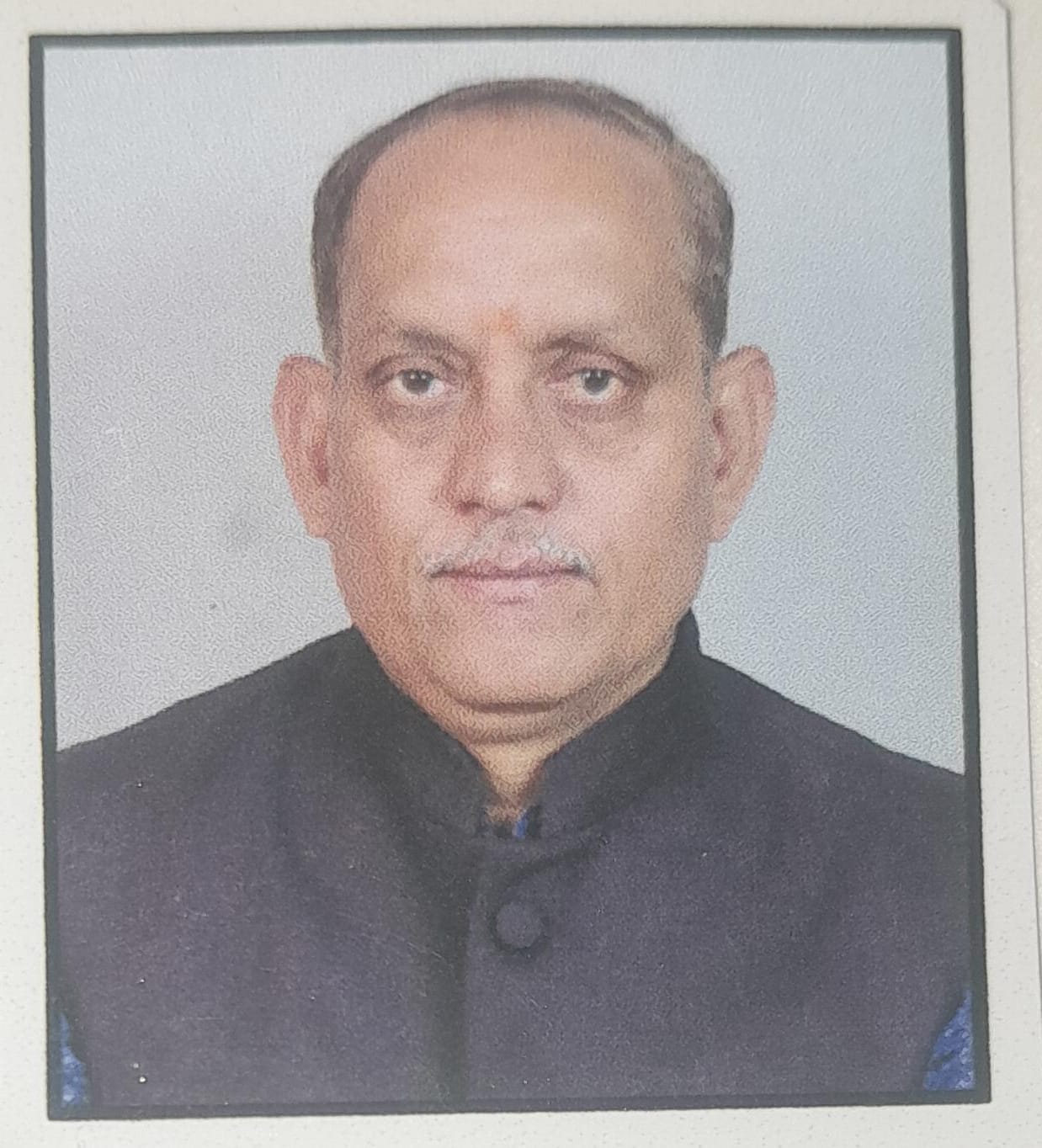
Leave a Reply